नाटक लेखन पर संक्षिप्त लेख लिखिये।Write a short article on play writing.
नाटक सृजनात्मक लेखन की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। अन्य विधाएँ श्रव्य मात्र हैं। नाटक या नाट्य चाक्षुष यज्ञ या दृश्यकाव्य के रूप में जाना जाता है। यह दृश्य भी है और काव्य भी। इसका ‘साहित्य’ तत्त्व उतना ही अनिवार्य है जितना ‘दृश्य’ तत्त्व। ‘दृश्यं श्रव्यं च यद्भवेत।’
(नाट्यशास्त्र 1/11) नाटक की रचना ही ‘नाट्य’ या ‘प्रस्तुति’ के लिए होती है। ‘रंग’ तत्त्व उसका अपरिहार्य पक्ष है। पाठ्य रूप (आलेख) में भी बिम्बधर्मिता उसका आधार है। नाटक बिम्बधर्मी विधा है- इसलिए वह समस्त काव्य में रमणीय है। नाटक लिखना सरल नहीं जटिल कार्य है। अच्छा नाटक लिखना और भी कठिन कार्य है।
प्रायः बहस होती है कि रेडियो नाटक श्रेष्ठ है या रंगनाटक ? रेडियो नाटक केवल श्रव्य है और अमूर्तता से सम्पन्न। इसकी श्रव्यता मानस-दृश्यों की सम्भावना का विस्तार करती है। रंगनाटक अपेक्षाकृत स्थूल है। आँखों और कानों से ग्रहण किये जाने वाले बिम्बों का स्वरूप सीमित कर देता है। फिर भी रंगनाटक दृश्य और श्रव्य दोनों ही माध्यमों की शक्ति से सम्पन्न त्रिआयामी कला है।
रंगनाटक का दर्शकों के साथ जो प्रत्यक्ष और सजीव सम्बन्ध बनता है, वह फिल्म का नहीं बन पाता। दर्शकों से सजीव सम्बन्ध ही फिल्म से तात्विक रूप से नाटक के अन्तर को स्थापित करता है। इसीलिए यह फिल्म या टेलीनाटक से अधिक रमणीय है। रंगनाटक का माध्यम अभिनेता है, पर वह दर्शक पर केन्द्रित होता है। काव्य या आलेख रूप में भी वह ‘दृश्यकाव्य’ है-जिसे दर्शक के लिए ही रचा जाता है। रंग प्रक्रिया की सम्पूर्णता में वह स्वयं भागीदार बनता है। नाटक दर्शकों के सम्मुख प्रदर्शन के लिए ही लिखा जाता है- रचा जाता है।
वह दर्शकधमीं है। फिल्म पूर्व निर्मित होती है। दर्शक उसे कैमरे की आँख से देखता है। रंगधर्मी होना नाटक (आलेख) की नियति है। दर्शक के बिना उसकी कल्पना भी सम्भव नहीं। उसके लिए शब्द के केन्द्र में अभिनेता रहता है जो प्रस्तुति का माध्यम भी है। शब्द उसके माध्यम से साकार होते हैं; स्थूल रूप ग्रहण करते हैं। पर नाटक का अपना स्थापत्य या संरचना-तत्त्व भी विलक्षण और अद्भुत है।

संक्षेप में रंगमंच के प्राइमर को अंग्रेजी के तीन ‘ए’ (A) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। Actor (अभिनेता) Audience (प्रेक्षक) और Architecture (स्थापत्य या संरचना)। अभिनेता (Actor) रंगमंच का केन्द्रीय घटक है। अपने व्यापक अर्थ में रंग प्रस्तुति से जुड़े सभी कलाकारों की कला के समुच्चय को संकेतित करता है। अभिनेता सहित अन्य कलाकार अपनी कला के योग से नाटककार के शब्दों को जीवन प्रदान करते हैं। प्रेक्षक सिर्फ मूक दर्शक मात्र नहीं – वह रंगमंच पर निर्मित सूक्ष्म-स्थूल बिम्बों और नाट्यार्थ को ग्रहण करता है। आलेख में भी यह रंग परिकल्पना निहित है। जो अनकहा-अधकहा अथवा मौन द्वार ध्वनित सम्वेदना को भी अपनी क्षमता अनुसार ग्रहण करता है। अभिनेता और नाटककार की कला उसे ही सम्बोधित है। पश्चिम में विरेचन उसे ही लक्ष्य करके ध्वनित है। भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार नाट्य का रसास्वादन भी वही करता है। नाटक के स्थापत्य (Architecture) से तात्पर्य है-उसकी संरचना करने वाले अनिवार्य तत्त्व। जो भवन-निर्माण में ईंट-गारे के समान उसके निर्माण में सहायक होते हैं। कथानक, चरित्र, संवाद (भाषा-शैली सहित) और रंगकर्म या रंग पक्ष इसी रूप में लिए जा सकते हैं।
नाटक दृश्य-बिम्बों में घटित होता है। दृश्य का नाटक में बहुत महत्त्व है। एक समय में एक ही स्थान पर जितना कुछ घटित होता है- उसे दृश्य कहते हैं। इसीलिए; (क) नाटक या एकांकी में स्थान और काल के संकेत परिवेश-निर्माण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।
(i) नाटक सदा वर्तमान काल में घटित होता है। इसीलिए वर्तमानकाल में लिखा जाता है।
(ii) नाट्य-स्थितियाँ या घटना क्रम इस रूप में लिखे जाएँ कि पढ़ते ही पूरा दृश्य बन
(iii) काल और स्थान का पूरा दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाए। घटना कहाँ घटित हुई (दिन या रात, शाम या प्रातः आदि में), कैसे घटित हुई, इसका परिचय दृश्य में दिया जाता है। वह क्रिया-व्यापार के अतिरिक्त वेशभूषा और रंगोपकरणों के माध्यम से भी उपस्थित होता है।
ख) घटना या स्थिति को संवाद या बातचीत के रूप में लिखा जाना चाहिए।
(i) संवाद प्रथम पुरुष के रूप में लिखे जाते हैं- मैं जा रही हूँ, मैं घर चला आया। मैं गया।
(ii) कैसे बोला जाए- यह भी निर्देशित होता है। क्रोध से, आश्चर्य से, पार्श्व से (जो मंच पर उपस्थित न हो, तब भी आवाज़ सुनाई दे, जाता है, झाँकता है) सम्बन्धी क्रिया- व्यापार भी निर्देशित होते हैं। नाटक में कैसे बोला जाए का निर्देश अनिवार्य न भी हो, अभिनय में सहायक होता है। नाटककार की रंगपरिकल्पना को समझने में सुविधा होती है। पर न भी हों तब भी नाटक की प्रकृति पर आघात नहीं होता। हाँ नाट्य-भाषा अभिनय-भंगिमाओं को स्पष्ट झलकाती हो। संस्कृत नाटकों में अभिनय निर्देश प्रायः अत्यल्प ही रहे। कुशल अभिनेता संवादों के खोल के भीतर छिपे कार्य-व्यापार और अभिनय-भंगिमाओं का सन्धान स्वयं कर लेते हैं।
(ग) नाटक के तीन अंग मुख्य हैं- आदि, मध्य और अन्त। आरम्भिक भाग में पात्र परिचय दिया जाता है। नाटक में वर्णन नहीं- घटित होता या दिखाया जाता है। अथवा सूच्य या संकेतित होता है। पात्र संख्या कम होनी चाहिए। वे क्या चाहते हैं, उनकी समस्या क्या है? आरम्भ में ही इसका परिचय मिल जाए तो उत्सुकता बनी रहती है। मध्यभाग में घटनाओं और स्थितियों का जाल बन जाता है। पात्रों के विचार या क्रिया-व्यापार उलझन उत्पन्न करते हैं। अन्त में उन समस्याओं को सुलझाया जाता है। नाटक तेज़ी से अपने लक्ष्य या उद्देश्य की ओर बढ़ता है।

(घ) आदि, मध्य और अन्त की अन्विति में कथाबिन्दु और क्रियाबिन्दुओं का विशेष महत्त्व है। उनका निरन्तर ध्यान रखना जरूरी है। कथानक (Plot) विश्वसनीयता और त्वरा से क्रमशः आगे बढ़े। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है- बिल्कुल स्पष्ट हों। कथानक के मोड़ भी इसी तर्क-क्रम से सामने स्पष्ट हों। क्रिया बिन्दुओं (Action points) का नाटक में अपना महत्त्व है। ये नाटक के अनिवार्य घटक हैं- जो कार्यव्यापार और अभिनेता दोनों से सम्बन्धित हैं। क्रिया-व्यापारों से ही पात्रों का चरित्र उभरता और निखरता है। अपने ‘कर्मों’ से पात्र निरूपित होते हैं। नाटक के क्रिया-व्यापार ऐसे हों कि जो पात्रों के चरित्रों का उद्घाटन करते जाएँ। नाटक न भी लिखें तो चल सकता है, पर ‘क्रिया-व्यापार-बिन्दुओं के बिना नाटक’ नहीं चलेगा। एकांकी या नाटक निरन्तर जिज्ञासापूर्ण बना रहे। समाप्ति पर ‘आगे क्या हुआ’ जानने की इच्छा बनी रहे तभी नाटक प्रभावशाली बनता है। जिज्ञासापूर्ण बनकर Interval point पर एकांकी या नाटक का अन्त सघन प्रभाव बनाता है।
नाटक के चरित्रों का निर्माण जीवन की मिट्टी से – जीवन के खट्टे-मीठे अनुभवों से किया जाए। पात्र के अनुभव और लेखक के अनुभव दोनों मिल कर सहज और निर्मल रूप से चरित्र का निर्माण करें। पात्र कौन लोग हैं? उनके आपस में क्या सम्बन्ध हैं? अपने जीवन में कौन-सा पात्र, किस पात्र को, क्या महत्त्व देता है? प्रमुख पात्र कौन है? इनका सावधानी से परिचय देना चाहिए। पात्र का स्वभाव और वर्ग- दोनों (नाटक के) संवादों के माध्यम से और क्रिया-व्यापार से झलकें।
संवादों की भाषा मानकीकृत हो, उसमें सरसता और आर्द्रता होनी चाहिए। हर भाषा की अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव और चरित्र होता है। उसे बदलना नहीं चाहिए। भाषा की प्रकृति को बदलने से उसका सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। शब्दों और अर्थों की छवियाँ परस्पर सम्बद्ध होनी आवश्यक है। संवादों की गठन और भार्षिक भंगिमाओं में- पात्र का स्वभाव और वर्ग, उसकी मानसिकता की झलक होनी चाहिए। इसके लिए पात्र की रूपरेखा पहले से बना ली जाए। फिर रचनाकार अपने-पराए अनुभवों को काट छाँट कर अपनी बुद्धि से पात्रों को विश्वसनीयता दे। कल्पितं पात्र भी अनुभव की मिट्टी से बनाए जाए और बुद्धि की कैंची से आवश्यकतानुसार अनुभवों की काट-छाँट की जाए।
नाट्यरचना को लक्ष्य क्या है? नाटक क्यों लिखा जा रहा है ? इस बात को ध्यान में रखकर ही कथा-बिन्दु, क्रिया-व्यापार और पात्रों का संयोजन किया जाए। समस्या के कारण और विस्तारक बिन्दु आदि और मध्य में विशेष रूप से संकेतित हों। अन्त में उन्हें धीरे-धीरे समेट कर ‘लक्ष्य’ पूर्ति की ओर सहजता और विश्वसनीयता से बढ़ाया जाना चाहिए।
कथानक, चरित्र और संवाद नाट्य-संरचना (स्थापत्य) के अनिवार्य घटक हैं। किसी एक के स्खलन से नाटक का अस्तित्व ही न रहेगा। नाटक का कथ्य या उद्देश्य भी महत्त्वपूर्ण घटक है-जो रचनाकार को इस माध्यम विशेष से अपनी बात कहने के लिए विवश करता है। यदि चेतना का यह उद्देश्य न हो तो नाटककार नाटक ही न लिखेगा। कथ्य या उद्देश्य का सम्बन्ध नाटककार के जीवन-दर्शन से भी जुड़ता है।
कथानक, चरित्र, संवाद (भाषा) और कथ्य को यदि नाटक के अनिवार्य घटक माना जा सकता है, तो देशकाल और शैली नाटक की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रभविष्णुता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।
अभिनेताओं की क्षमता और अभिनय संभावनाओं, प्रेक्षकों की समक्ष और ग्राह्यता का निरंतर ध्यान रखकर ही नाटक को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
उपन्यास लेखन पर संक्षिप्त लेख लिखिये।Write a short article on novel writing.
उपन्यास – कविता और नाटक अगर साहित्य की परम्परागत विधाएँ मानी जाती हैं, तो उपन्यास नितान्त आधुनिक। 1605 ई. में प्रकाशित सर्वांतीज के उपन्यास ‘डॉन किहोटे’ को आमतौर पर पाश्चात्य परम्परा का पहला उपन्यास माना जाता है। अगर उससे उपन्यास की शुरुआत मानें तो उपन्यास को लिखे जाते चार सौ से अधिक वर्ष नहीं हुए हैं। लेकिन आज उपन्यास का जो रूप हमारे सामने है, विधा के रूप में उसकी पहचान 18वीं शताब्दी के यूरोप में बनी।
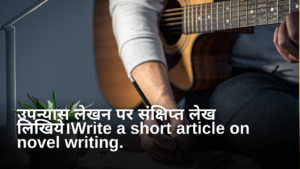
उपन्यास को सामान्य तौर पर यथार्थवादी विधा के रूप में देखा जाता है। उपन्यास के उद्भव को लेकर अनेक विचार रहे हैं, लेकिन यूरोप में उपन्यास के उद्भव को लेकर सामान्य तौर पर दो तरह की धारणाएँ प्रचलित रही हैं। एक विचार उपन्यास को बुर्जुआ वर्ग के उदय और आधुनिक पूँजीवाद से उद्भव से जोड़कर देखता रहा है दूसरा विचार जो उपन्यासों के उद्भव और विकास को लेकर यूरोप में देखता रहा है। बहरहाल, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के दौर में चार्ल्स डिकेंस, डब्ल्यू. एम. ठाकरे, सर वाल्टर स्कॉट जैसे उपन्यासकारों के सुदीर्घ उपन्यासों ने ही वह जमीनं तैयार की, जिसके आधार पर उपन्यास ने आगे विकास किया।
वास्तव में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और औद्योगिक क्रान्ति के कारण यूरोप में जो मध्य-वर्ग पैदा हुआ, उसे महाकाव्य या रोमांस जैसी विधाएँ सामन्ती मूल्यों में रची-बसी लगने लगीं। एक नया समाज बन रहा था, शहरों ने नयी जीवन-शैली का प्रचलन बढ़ रहा था। एक तरफ औद्योगिक समाज में काम करने वालों का जीवन था, उनका एकाकीपन था, लोग अपने- अपने गाँवों-परम्पराओं से कटकर जीविका के लिए दूसरे बड़े शहरों में जा रहे थे। यूरोप में उपन्यास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव के इसी सन्धिकाल की उपज है।
उपन्यास के रूप में नये समाज को एक ऐसी विधा मिली जिसमें वह बदलते समाज के ताने-बाने को हमेशा के लिए अंकित कर लेना चाहता था। राजा-महाराजाओं, सामन्तों के जीवन की कथाओं में आधुनिक मनुष्य की दिलचस्पी नहीं रह गयी थी। उपन्यास के रूप में उसे एक ऐसी विधा मिल गयी थी जिसमें वह महाकाव्यों की तरह अपने जीवन-संघर्ष को दर्ज कर सकता था। एक ऐसे दौर में जब पारम्परिक सामाजिकता खण्डित हो रही थी, लोग एकाकी रहने को अभिशप्त थे, वैसे दौर में उपन्यास ने एक प्रकार की सामाजिकता रचने का काम किया।
यह तो हुई बात यूरोप में उपन्यास के उद्भव और विकास के कारणों की ? लेकिन पौर्वात्य परम्परा में गद्य के कुछ ऐसे नमूने पहले से उपलब्ध रहे हैं, जिनको उपन्यास के पूर्व- प्रारूपों के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए बाणभट्ट ने सातवीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में ‘कादम्बरी’ की रचना की। दसवीं शताब्दी में जापान में गद्य की एक कथाकाव्य कृति की रचना हुई, जिसका अँग्रेजी अनुवाद “द टेल्स ऑफ जेंजी’, के रूप में विश्व भर में उपलब्ध है। इसके अलावा, भारत में पंचतन्त्र की कथा बाद में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गयी। इसी तरह फारसी परम्परा में अलिफ लैला है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या इन उपन्यास-पूर्व कथाख्यानों को उस रूप में उपन्यास माना जा सकता है जिस रूप में उपन्यास की विधा का पिछले 300-400 वर्षों में विकास हुआ है। इसका जवाब नकारात्मक ही होगा। आधुनिक उपन्यासों में ‘एक समय की कथा’ नहीं कही जाती है, बल्कि उसमें देशकाल की एकता होती है। इसके अलावा, जो एक बड़ा अन्तर इन पुराने कथारूपों और आज के उपन्यासों में दिखायी देता है वह यह है कि आज उपन्यास के केन्द्र में मनुष्य है, उसमें मनुष्य के जीवन का चित्रण होता है। हिन्दी में उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति से भी यही सिद्ध होता है कि वह मनुष्य की अभिव्यक्ति की सबसे नजदीकी विधा है। उपन्यास शब्द उप (नजदीक) और न्यास (थाती) से मिलकर बना है। हिन्दी में यथार्थवादी उपन्यास की धारा को सुस्थापित करने वाले लेखक प्रेमचन्द ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए भी लगभग यहीं बातें उसकी प्रकृति को लेकर कहीं हैं- ‘मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्रमाला समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है।…. आदमियों के चरित्रों में भी बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ विभिन्नताएँ भी होती हैं। यही चरित्र सम्बन्धी समानता और विभिन्नता-अभिनत्व में भिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिनव-दिखाना उपन्यास का मूल कर्तव्य है।’
इसके विपरीत व्यक्तिवादी उपन्यास के विचार के मानने वाले विचारक भी यह तो मानते ही रहे हैं कि उपन्यास का सम्बन्ध मनुष्य के जीवन से होता है, उसके परिवेश से होता है। लेकिन उनके यहाँ यह जीवन कुछ अधिक सूक्ष्म हो जाता है। प्रसिद्ध उत्तर आधुनिक उपन्यासकार मिलाना कुंन्देरा ने अपनी पुस्तक ‘द आर्ट ऑफ नॉवेल’ में उपन्यास को परिभाषित करते हुए कहा है- उपन्यास, चाहे वह किसी भी दौर का हो, का सम्बन्ध आत्मा से होता है। जैसे ही शब्दों के माध्यम से आप कोई काल्पनिक चरित्र खड़ा करते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, तो अकस्मात आपके सामने यह प्रश्न उठ खड़ा होता है- आत्मा क्या है ? उसको किस चरित्र में ढाला जाए? इसी बुनियादी संवाल पर उपन्यास टिका होता है।
बहारहाल, यह तो हुई उपन्यास के उद्भव, विकास और उसकी प्रकृति सम्बन्धी बातें। इससे उपन्यास की जो सबसे बड़ी विशेषता उभर कर आई वह यह कि इसका सम्बन्धं
मानव, उसके जीवन, उसकी परिस्थिति से रहा है। इसीलिए समाज में जो भी बदलाव आये हैं, उपन्यास ने भी उतने ही रूपाकार ग्रहण किये हैं। इस रूप में उपन्यास को सबसे लचीली विधा कहा जाता है। आज अँग्रेजी में ‘ग्राफिक नॉवेल’ यानी चित्रित उपन्यास भी लिखे और पढ़े जा रहे- हैं। लेकिन इन सारे बदलावों के बीच उपन्यास की कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएँ हैं जिनके आधार पर किसी रचना को उपन्यास कहा जा सकता है। वैसे अपवाद हर पहलू के होते हैं।
Important Link
- पाठ्यक्रम का सामाजिक आधार: Impact of Modern Societal Issues
- मनोवैज्ञानिक आधार का योगदान और पाठ्यक्रम में भूमिका|Contribution of psychological basis and role in curriculum
- पाठ्यचर्या नियोजन का आधार |basis of curriculum planning
राष्ट्रीय एकता में कौन सी बाधाएं है(What are the obstacles to national unity) - पाठ्यचर्या प्रारुप के प्रमुख घटकों या चरणों का उल्लेख कीजिए।|Mention the major components or stages of curriculum design.
- अधिगमकर्ता के अनुभवों के चयन का निर्धारण किस प्रकार होता है? विवेचना कीजिए।How is a learner’s choice of experiences determined? To discuss.
- विकास की रणनीतियाँ, प्रक्रिया के चरण|Development strategies, stages of the process
Disclaimer: chronobazaar.com is created only for the purpose of education and knowledge. For any queries, disclaimer is requested to kindly contact us. We assure you we will do our best. We do not support piracy. If in any way it violates the law or there is any problem, please mail us on chronobazaar2.0@gmail.com






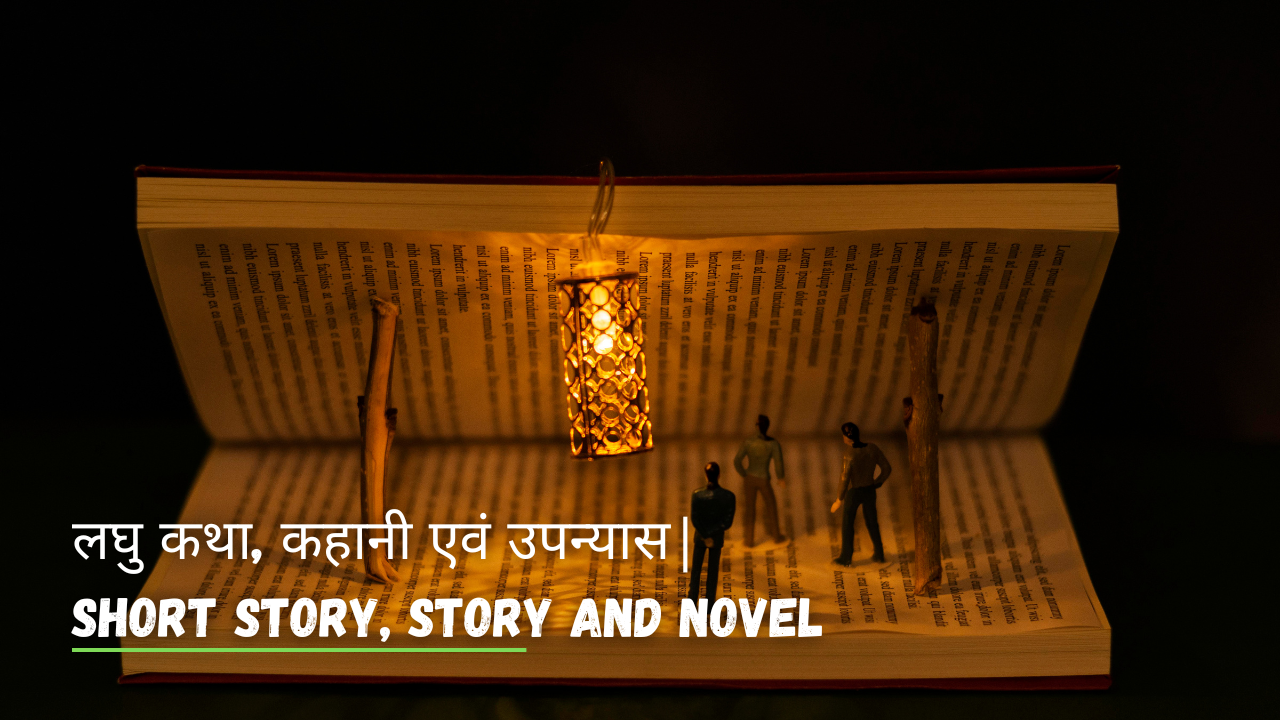






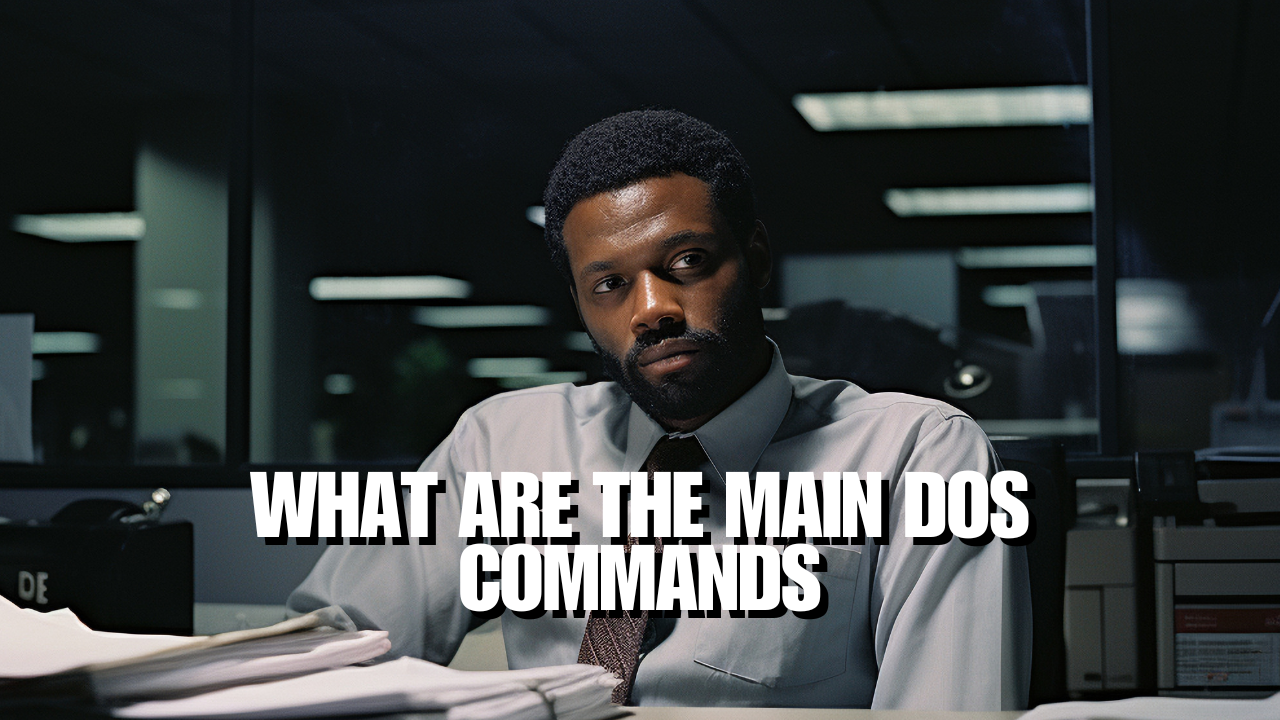
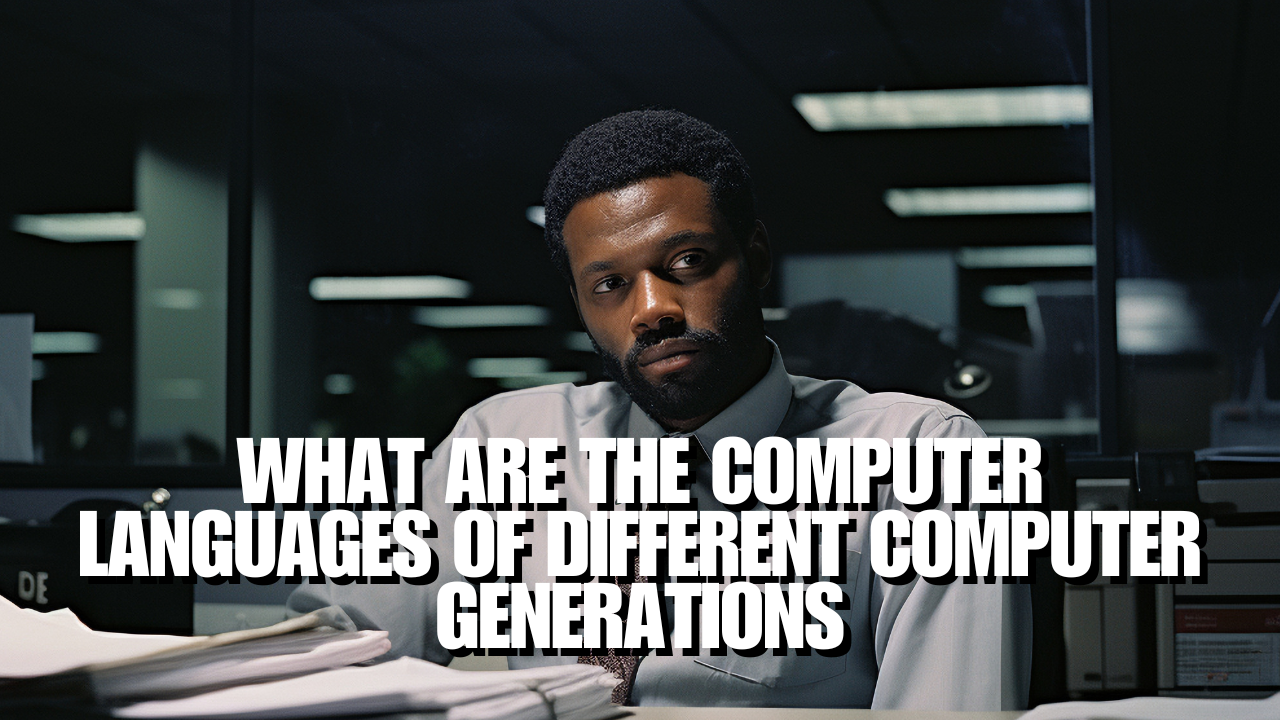

Leave a Reply