हिन्दी का विकास|development of hindi
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के द्वारा ही वह समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। भारत में भौगोलिक एवं सामाजिक विविधताओं के कारण अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। महात्मा गाँधी ने कहा भी है- “राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है।”
हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है, किन्तु व्यावहारिक रूप से इसे यह सम्मान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। हिन्दी को उसका वास्तविक सम्मान नहीं दिए जाने का मुख्य कारण भाषावाद है। भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हैं। इन सभी भाषाओं में हिन्दी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज देश में हिन्दी बोलने वालों की संख्या 42 करोड़ से भी अधिक है। भाषा की बहुलता का ही नतीजा है कि देश में भाषावाद की स्थिति उभरी है, जिससे हिन्दी को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि हिन्दी को राजभाषा का वास्तविक सम्मान मिले। वे इसका विरोध करते रहते हैं।
स्वतंत्रता आन्दोलन के समय राजनेताओं ने यह महसूस किया था कि हिन्दी, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की सम्पर्क भाषा है। देश के विभिन्न भाषा-भाषी आपस में विचार- विनिमय करने के लिए हिन्दी का सहारा लेते हैं। हिन्दी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था।
हिन्दी, राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो अत्यन्त सरल हैं। हिन्दी में आवश्यकतानुसार देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात् करने की शक्ति है और देशवासियों में भावात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है।
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में- “हिन्दी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है, जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।”

14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया था, इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को ‘हिन्दी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। ‘हिन्दी दिवस’ मनाए जाने का उद्देश्य इसका व्यापक प्रचार-प्रसार एवं राजकीय प्रयोजनों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। हर वर्ष सरकारी प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में धूमधाम से हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाता है और लोग हिन्दी में कार्य करने की शपथ लेते हैं। इससे न सिर्फ हिन्दी को बढ़ावा मिला, बल्कि लोगों में हिन्दी के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। वर्तमान समय में, हिन्दी ने विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल ने ‘भाषा शोध अध्ययन-2012’ में यह सिद्ध किया कि हिन्दी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसने अंग्रेजी सहित विश्व की अन्य भाषाओं को भी इस मामले में पीछे कर दिया है। यदि हम हिन्दी की संवैधानिक स्थिति की बात करें, तो आजादी से पहले जो छोटे-बड़े नेता राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर-हिन्दी भाषी नेता स्वतन्त्रता मिलने के समय हिन्दी के नाम से दूर भागने लगे और फिर स्थिति यह बनी कि संविधान सभा में केवल हिन्दी पर विचार न कर अंग्रेजी सहित संस्कृत एवं हिन्दुस्तान की अन्य भाषाओं पर भी विचार किया गया।
संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिन्दी और अंग्रेजी के समर्थकों में देखने को मिली, हालाँकि आज़ाद भारत में एक विदेशी भाषा, जिसे यहाँ के मुट्ठीभर लोग पढ़-लिख एवं समझ सकते थे, देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी, लेकिन अंग्रेजी को यूँ छोड़ा भी नहीं जा सकता था। ऐसे में हिन्दी पर ही विचार किया गया वैसे यह देश की 46% से अधिक जनता की भाषा थी। इन सब बातों पर गौर करते हुए संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि राजभाषा बनाया जाए। आचार्य विनोबा भावे ने एक बार कहा भी था- “मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज़्ज़त करता हूँ, पर मेरे देश में हिन्दी की इज़्ज़त न हो यह मैं नहीं सह सकता।”
आज हिन्दी भारत की राजभाषा है। राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने एवं इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है, जिनमें कक्षाओं, कवि सम्मेलनों, नाटकों, संगोष्ठियों, हिन्दी अनुसंधानों, हिन्दी-टंकण आदि को बढ़ावा देने के साथ- साथ हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता दिया जाना प्रमुख है। वहीं कम्प्यूटर, इण्टरनेट, ई-बुक, विज्ञापन, टेलीविजन, रेडियो आदि क्षेत्रों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करके इसके विकास एवं संवर्द्धन का कार्य किया है।

देश के युवाओं ने भी नए-नए स्तरीय लेखों द्वारा इसे उच्च शिखर पर पहुँचाया है। हिन्दी को आज भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली है। मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका आदि देशों में हिंदी बोली व समझी जाती है। आज विश्वभर में 10 जनवरी को ‘विश्व हिन्दी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है और समय-समय पर ‘विश्व हिन्दी सम्मेलन’ का आयोजन किया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा ओमान स्थित भारतीय दूतावास में 10 जनवरी, 2018 को विश्व हिन्दी दिवस मनाया गया। दसवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन वर्ष 2015 में भोपाल (म.प्र.) में सम्पन्न हुआ तथा 11वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन वर्ष 2018 में मॉरिशस में होना प्रस्तावित है। यह सम्मेलन हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर को आयोजित होता है। विश्व में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन आरम्भ किया गया। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। आज हिन्दी की इन सारी उपलब्धियों को देखकर पं. गोविन्द वल्लभ पन्त की कहीं यह बात सत्य साबित होती है- “हिन्दी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता।”
सरकार द्वारा समय-समय पर राजभाषा हिन्दी के सन्दर्भ में जारी आदेशों का अनुपालन करने के लिए गृह मन्त्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन जून, 1975 में किया गया था। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और प्रयोग से जुड़ी राजभाषायी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना इस विभाग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आठ क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं। राजभाषा के रूप में हिन्दी को उचित स्थान पर विराजमान करने के उद्देश्य से समय-समय पर कई समितियों का गठन किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति, केन्द्रीय हिन्दी समिति, हिन्दी सलाहकार समिति, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इत्यादि कुछ ऐसी ही समितियाँ हैं।

हिन्दी आज भारत की एक प्रमुख सम्पर्क भाषा है। कुछ लोग अंग्रेज़ी को भारत की सम्पर्क भाषा कहते हैं, किन्तु ऐसा कहते हुए वे भूल जाते हैं कि अंग्रेज़ी देश के आम आदमी की भाषा न कभी थी और न कभी हो पाएगी। हिन्दी भारत की एक ऐसी भाषा है, जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषा-भाषी आपस में अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। पश्चिम बंगाल का एक बांग्लाभाषी व्यक्ति दिल्ली के हिन्दीभाषी व्यक्ति से हिन्दी में ही बात करता नज़र आता है। पंजाब के पंजाबी बोलने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लोगों से बात करने के लिए हिन्दी का सहारा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं एक गुजराती बोलने वाला व्यक्ति यदि पश्चिम बंगाल जाता है, तो उसे सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का ही सहारा लेना पड़ता है।
ऐनी बेसेण्ट ने बिल्कुल सत्य कहा है- “भारत के विभिन्न प्रान्तों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में जो भाषा सबसे प्रभावशाली बनकर सामने आती है वह है हिन्दी। वह व्यक्ति, जो हिन्दी जानता है, पूरे भारत की यात्रा कर सकता है और हिन्दी बोलने वालों से हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है।” बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार हिन्दी में ही करना पड़ता है।

अंग्रेज़ी एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है, जो बड़ी-बड़ी कम्पनियों एवं विदेशों में अच्छे रोज़गार प्राप्त करने का माध्यम बन चुकी है, लेकिन इस कारण से हिन्दी के अपमान एवं इसकी अवहेलना को तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकात। हिन्दी देश को भावानात्मक एकता के सूत्र में बाँधने में सक्षम भारत की एकमात्र भाषा है, इसलिए इसे राजभाषा का वास्तविक सम्मान दिए जाने की आवश्यकता है। हिन्दी की प्रगति हेतु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की पंक्तियाँ आज भी उल्लेखनीय हैं
“निजभाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल ॥
अंग्रेजी पढ़ि-पढ़ि भये केते लोग प्रवीन ?
पै निज भाषा ज्ञान के रहे हीन के हीन।।”
Important Link
- पाठ्यक्रम का सामाजिक आधार: Impact of Modern Societal Issues
- मनोवैज्ञानिक आधार का योगदान और पाठ्यक्रम में भूमिका|Contribution of psychological basis and role in curriculum
- पाठ्यचर्या नियोजन का आधार |basis of curriculum planning
राष्ट्रीय एकता में कौन सी बाधाएं है(What are the obstacles to national unity) - पाठ्यचर्या प्रारुप के प्रमुख घटकों या चरणों का उल्लेख कीजिए।|Mention the major components or stages of curriculum design.
- अधिगमकर्ता के अनुभवों के चयन का निर्धारण किस प्रकार होता है? विवेचना कीजिए।How is a learner’s choice of experiences determined? To discuss.
- विकास की रणनीतियाँ, प्रक्रिया के चरण|Development strategies, stages of the process
Disclaimer: chronobazaar.com is created only for the purpose of education and knowledge. For any queries, disclaimer is requested to kindly contact us. We assure you we will do our best. We do not sup

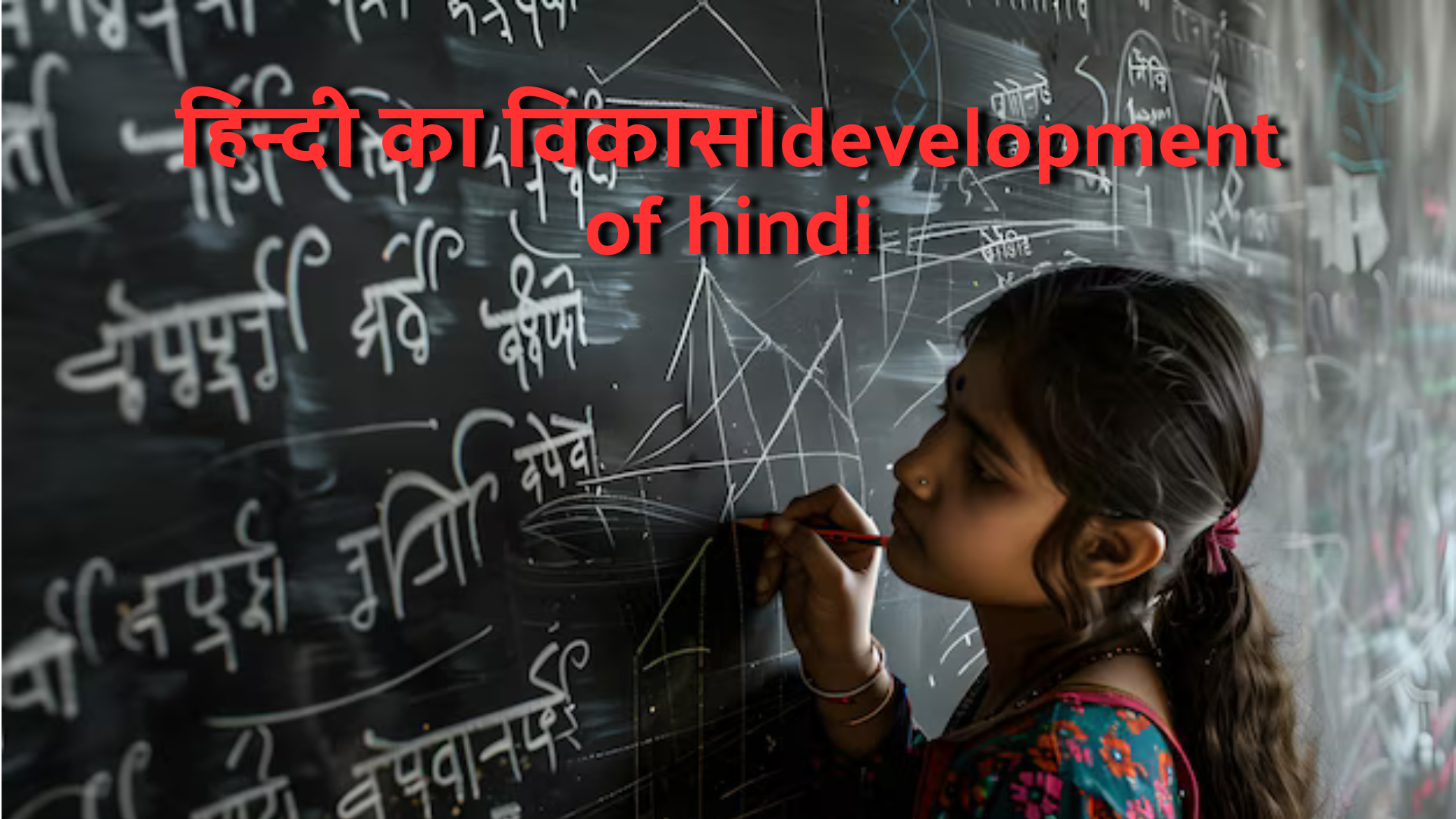

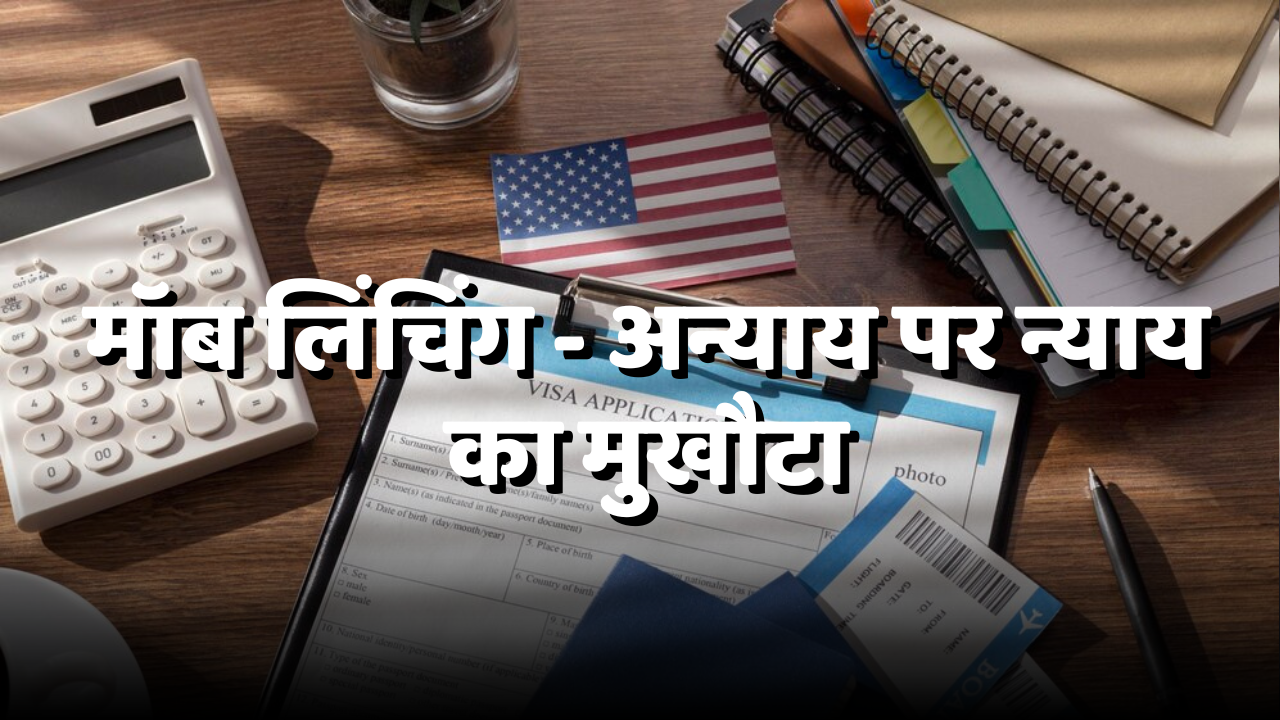

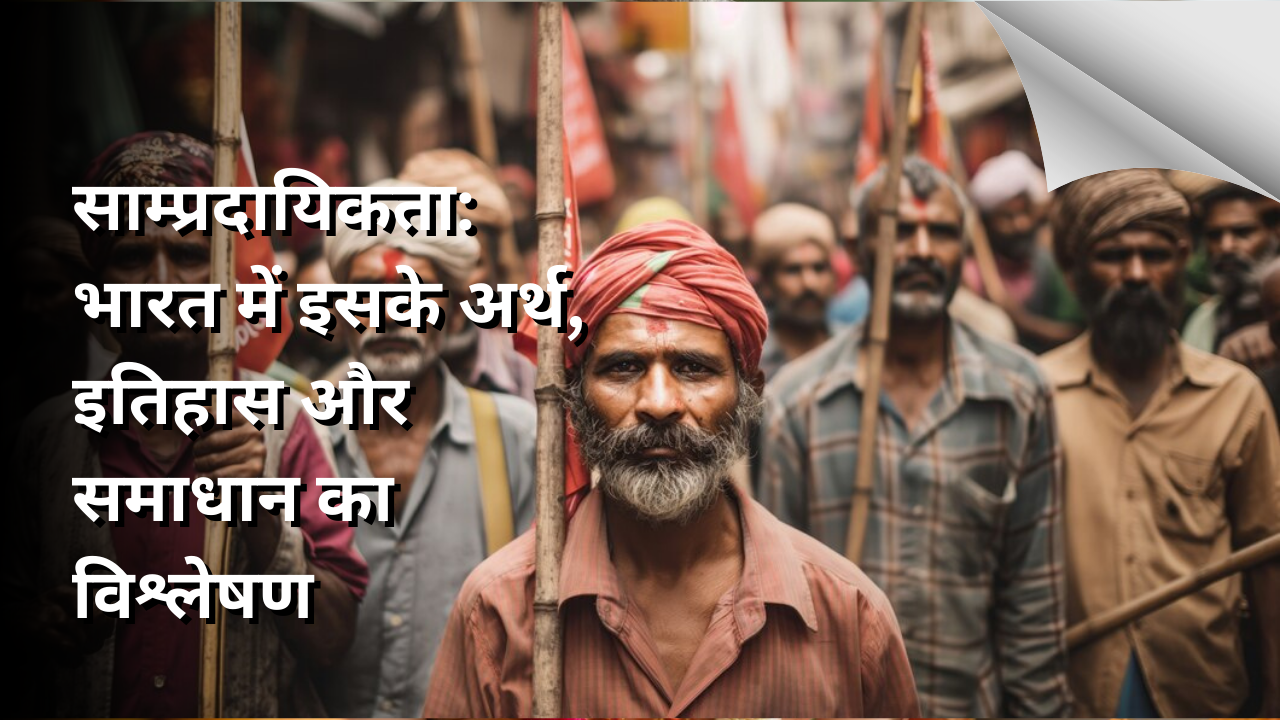



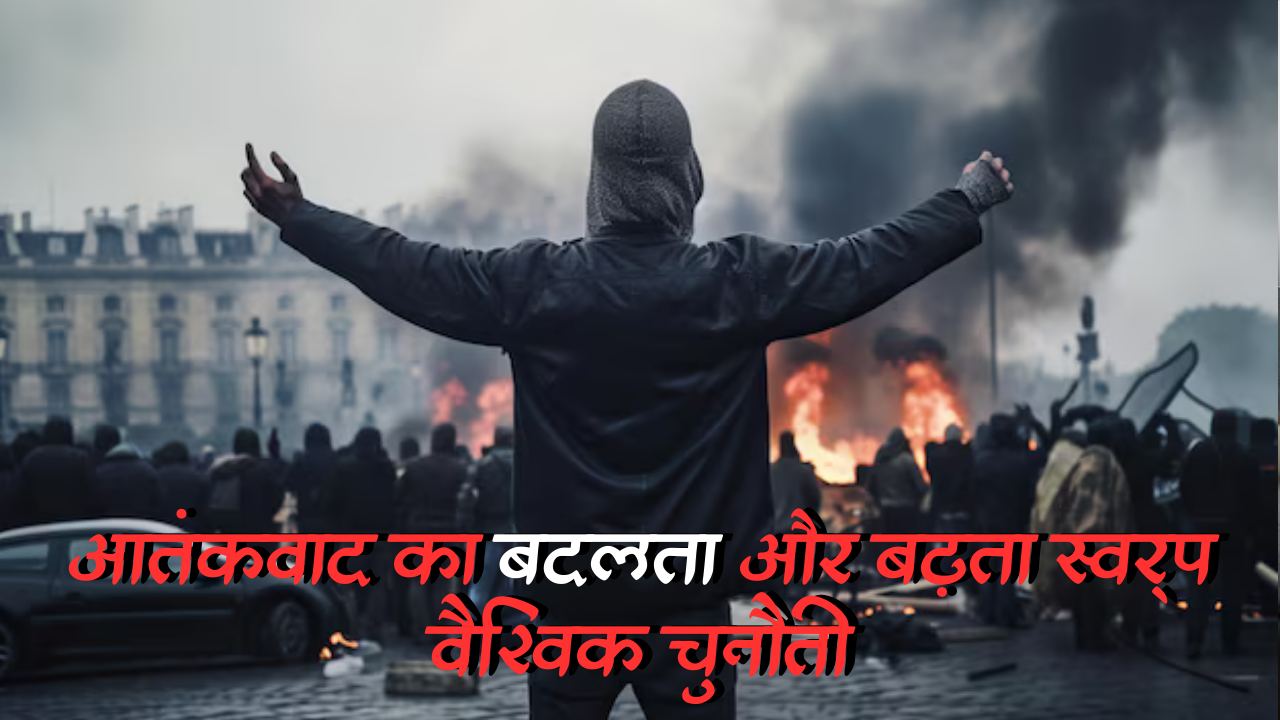
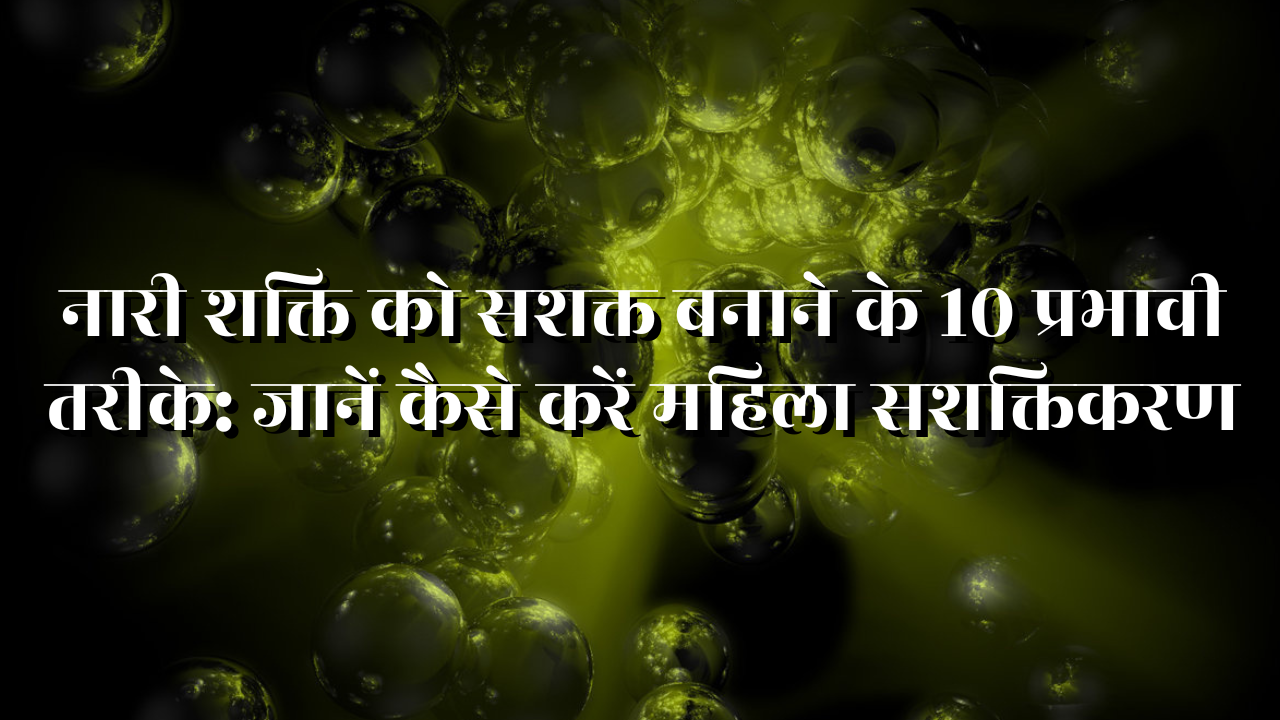
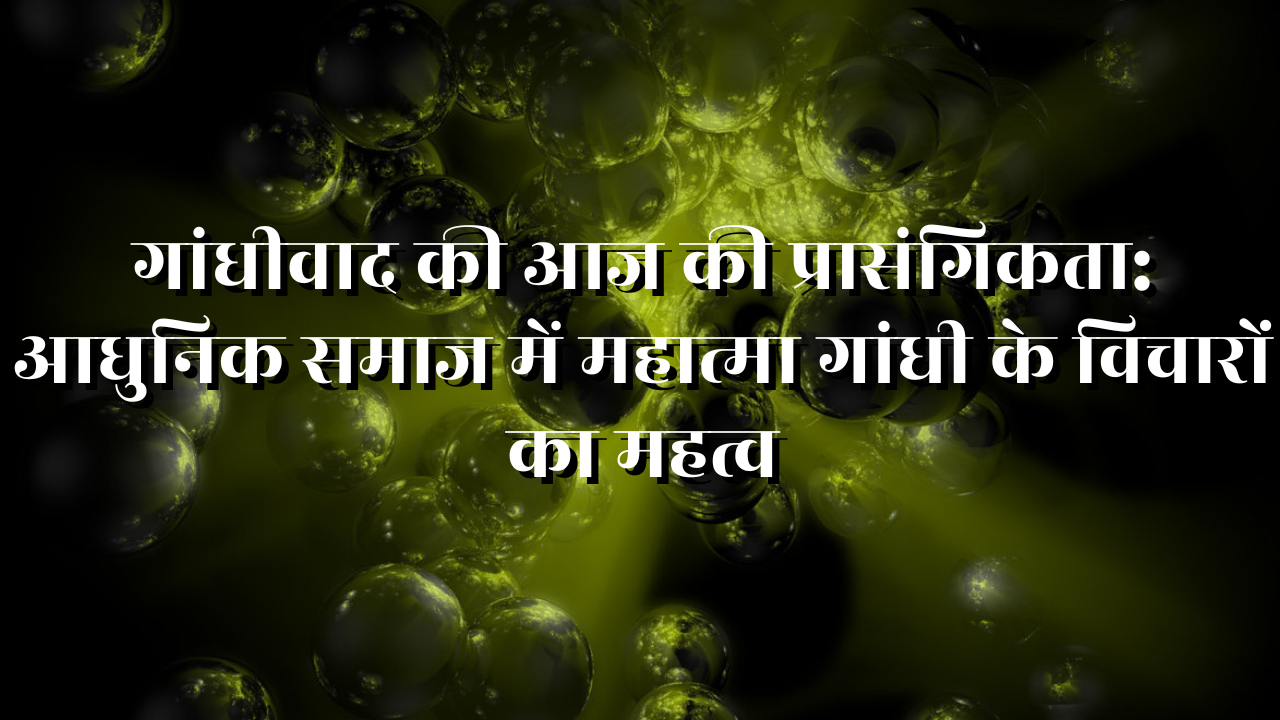

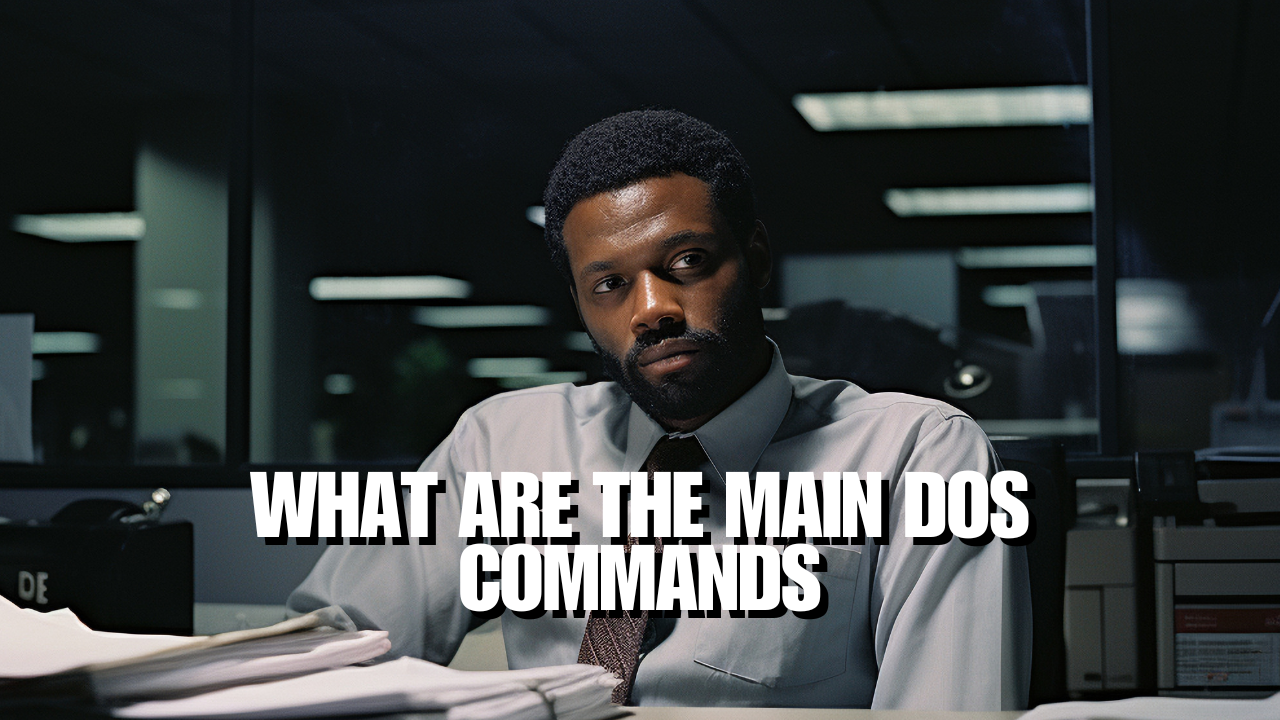
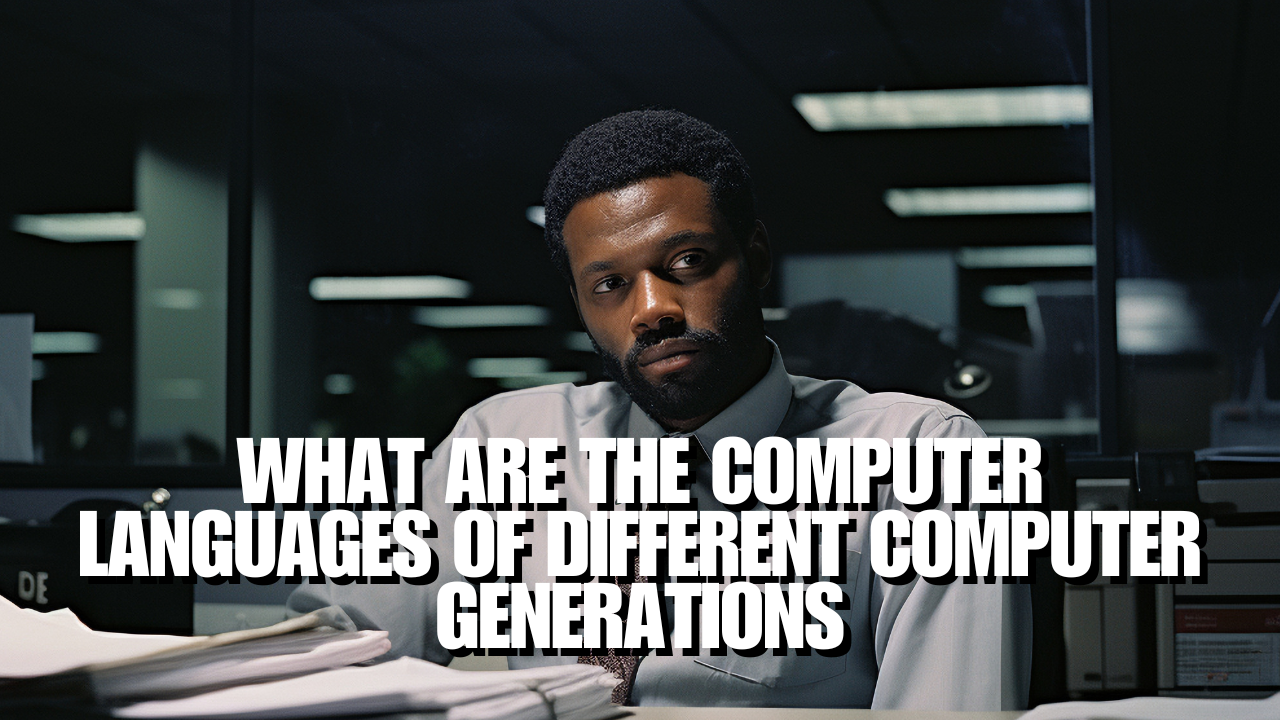

Leave a Reply