बुलेट ट्रेनः सुनहरे भविष्य की ओर एक कदम|Bullet Train: A step towards a bright future
भारत में 165 वर्ष पूर्व 16 अप्रैल, 1853 को 33.81 करोड़ किलोमिटर लम्बे मार्ग पर मुम्बई से ठाणे के बीच 8 किलोमिटर प्रति घण्टे की रफतार से पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। आज विश्व के शीर्ष रेल नेटवर्क वाले पाँच देशों में शामिल है। कर्मचारियों की वृहत् संख्या के आधार पर भारतीय रेल विश्व की नौवीं सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था है। भारतीय रेल ने उत्तरोत्तर विकास करते हुए और नई तकनीक को आत्मसात् करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भारतीय रेल के विकास की अगली कड़ी बुलेट ट्रेन है। इसमें रफतार भी है और सुरक्षा भी है। रफतार भारतीय जनमानस को रोगामच से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अहमदाबाद में साबरमती के पास देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशीला रखी। भारत सरकार ने यह परियोजना जापान की सहायता से शुरू की है तथा 15 अगस्त, 2022 को ट्रेन के परिचालन का लक्ष्य रखा गया है। भारत में हम जिसे बुलेट ट्रेन कहते हैं, जापान में वह शिनकानसेन कहलाती है।
शिनकानसेन या बुलेट ट्रेन
जापान में बुलेट ट्रेन की परिकल्पना 19वीं सदी में ही रख दी गई थी, लेकिन लगातार दो विश्व युद्धों के कारण यह क्रियाशील नहीं हो पाई। 1930 के दशक में डंगन रेशा के नाम से शुरूआत करने की काशिश की गई पर यह परियोजना चल नहीं पाई। डंगन रेशा का शाब्दिक अर्थ बुलेट ट्रेन है। बाद में 1940 के दशक में जब इसे दोबारा शुरू किया गया, तब इसका नाम शिनकानसेन रखा गया। 1 अक्टूबर 1964 में टोक्यो ओलम्पिक के समय पहली शिनकानसेन ट्रेन चली। जिसका आविष्कार जापान के हिड्यो शाइमा ने किया था। इसने टोक्यो से ओसाका की लगभग 500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ चार घण्टे में पूरी में पूरी कर ली। अब तो यह दूरी ढाई घण्टे में तय हो जाती है। वर्तमान में विश्व के मात्र 15-16 देशों में बुलेट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है जिसमें चीन 27,000 किमी नेटवर्क के साथ प्रथम स्थान पर है। अन्य देशों में स्पेन, फ्रांस और जर्मनी आदि देश शामिल हैं।
अपनी बेहतरीन तकनीक की वजह से शिनकानसेन ग्लोबल ब्रैण्ड बन चुका है। जापान से भारत को बुलेट ट्रेन की सबसे बेहतरीन और सुरक्षित शिनकानसेन तकनीक मिलेगी और वाहन संचालन एवं रख-रखाव का भी प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए वडोदरा में एच.एस.आर. संस्थान (हाई स्पीड रेल) स्थापित करने की योजना बनाई जा चुकी है।
भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना की तथ्यात्मक जानकारी
पहले चरण में शिनकानसेन ट्रेन मुम्बई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अहमदाबाद और मुम्बई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की कुल लागत रु 1,10,000 करोड़ (17 बिलियन डॉलर) का अनुमान है। जापान इस परियोजना के लिए कुल लागत का 81% अथार्त रु 88,000 का कर्ज देगा। जापान ने यह धनराशि 0.1% वार्षिक ब्याज की दर पर 50 वर्ष के लिए कर्ज के तौर पर दी है और कर्ज वापस करे की शुरूआत 15 साल के भीतर करनी होगी। ब्याज को जोड़कर गणना करें, तो रु 88,000 के कर्ज के बदले भारत को रु 90,500 करोड़ चुकाने होंगे। इस रूट पर चलने वाली बुलेट ट्रेन कैसी होगी और उसमें क्या-क्या विशेषताएँ होंगी, इस पर भी जापान इण्टरनेशनल कॉपेरिशन एजेन्सी (जेआईएसीए) ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, बुलेट ट्रेन मुम्बई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमिटर की दूरी चार स्टेशनों पर रूकते हुए केवल 2 घण्टे 7 मिनट में तय करेगी।

मुम्बई और अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं- बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनन्द अहमदाबाद और साबरमती। यदि बुलेट ट्रेन इन 12 स्टेशनों पर रूकती है, तो मुम्बई और अहमदाबाद के बीच की दूरी को 2 घण्टे 58 मिनट में तय करेगी। इस रूट पर बुलेट ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घण्टा और अधिकतम स्पीड 350 किलोमिटर प्रति घण्टा होगी। शुरूआत में इस रूट पर प्रतिदिन एक दिशा में 35 ट्रेनें चलेंगी, जिसे वर्ष 2053 में 105 ट्रेनें प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है।
508 किलोमिटर लम्बे इस रूट का 92% हिस्सा एलिवेटेड, 6% सुरंग और नाकी 2% जमीन पर होगा अर्थात् 508 किलोमिटर में 468 किलोमीटर सुरंग के अन्दर और बाकी 13 किलोमीटर सुरंग के अन्दर और बाकी 13 किलोमीटर जमीन पर होगा। 10 कार इंजन वाली इस ट्रेन में 750 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। भविष्य में इसे 16 कार इंजन वाली बुलेट ट्रेन में बदलने का प्रस्ताव भी जे आईसीए की रिपोर्ट में दिया गया है, जिसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। प्रारम्भ में प्रतिदिन लगभग 36,000 लोग बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे तथा वर्ष 2053 तकं इसमें सफर करने वालों की संख्या प्रतिदिन 1,86,000 तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया है।
बुलेट ट्रेन सुनहरे भविष्य की ओर (लाभ)

भारत आने वाले 25 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना संजोए हुए है। वह पहले ही परमाणु ताकत से लैस है और अन्तरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में इसने विश्वसनीय प्रगति की है और अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में एचएसआर नेटवर्क वाले देशों के विशेष क्लब में शामिल होने का भारत का यह प्रयास अत्यन्त सराहनीय है, जिसने भारतीय परिवहन को एक नई उड़ान दी है।
एचएसआर के साथ-साथ नए उत्पादन अड्डों और टाउनशिप को भी विस्तारित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक सस्ते आवासों, लॉजिस्टिक्स केन्द्रों और औद्योगिक इकाइयों के खुलने से छोटे कस्बों और शहरों को भी लाभ होगा।
महाराष्ट्र के पालघर और गुजरात के वलसाड के साथ-साथ संघ राज्यक्षेत्र दमन में भी निवेश के नए अवसर निर्मित होंगे। बुलेट ट्रेन की निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों से इस्पात, सीमेण्ट और विनिर्माण जैसे सम्बद्ध उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके अतिरिक्त रसद एवं वसतुओं की भण्डारण सम्बन्धी माँग को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे निकट भविष्य में देश की आर्थिक उन्नति को स्थायी भी सहारा मिलेगा तथा देश में बहुत-सी नई एवं अस्थायी नौकरियाँ होंगी। अकेले निर्माण क्षेत्र में ही लगभग 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की सम्भावना है। परियोजना के संचालन के बाद ट्रेन की लाइनों के संचालन और रख-रखाव के लिए कम-से-कम 40,000 नौकरियों का सृजन किया जाएगा। साथ ही लगभग 16,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

इतना ही नहीं इस जटिल और वृहद् परियोजना का प्रबन्ध करना भारतीय एजेन्सियो के लिए भी एक बेहतर अनुभव साबित होगा, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अधिक-से-अधिक कौशल विकास होने की सम्भावना है। यदि वित्तीय बाधाओं से इतर, यह परिवहन के लिए एक नया आयाम है। यह एक अलग और विशिष्ट उपक्रम है, जो मेट्रो की तरह ही पारम्परिक रेलवे से अलग होगा। एचएसआर का वित्त एवं प्रबन्धन परम्परागत परम्परागत भारतीय रेलवे से अलग है। ऐसे में बुलेट ट्रेन का स्वागत भारत देश में किया जाना चाहिए।
वस्तुतः इस परियोजना की सफलता इसके निष्पादन पर निर्भर करती है। स्पष्ट है कि इस परियोजना को सफल तरीके से देश की स्वतन्त्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने अर्थात् वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना न केवल भारत में कुशल परियोजना कार्यान्वयन की संस्कृत विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करेंगी, बल्कि इससे परियोजना कार्यान्वयन के सन्दर्भ में परिदृश्य में भारत की छवि भी सुधरेगी। इसके लिए आवश्यक है कि भारत द्वारा इस परियोजना से सम्बन्धित कार्यों के शुरू होने से पहले इससे समबद्ध आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए, ताकि उसका समय पर कर्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यह भारत के लिए एक परिवर्तनकारी परियोजना साबित होगी।
भारत में बुलेट ट्रेन की राह में चुनौतियाँ
यद्यपि भारत में बुलेट ट्रेन की राह में चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। पलानिंग में बहुत कम समय देने के कारण परियोजना लम्बे समय तक बाधित रहती है। इस कारण परियोजना की लागत बहुत बढ़ जाती है। अतः मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना व्यवहार्यता की दृष्टि से चिन्ताजनक मानी जा रही है।
यह विदित है कि केवल विशिष्ट जनसांख्यिकी आय वाले देशों में ही बुलेट ट्रेन का सफल परिचालन सम्भव हो पाया है। इस कारण भारत में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बुलेट ट्रेन का किराया कहीं आम आदमी की पहुँच से बाहर न हो जाए, इसके लिए भारत में हमेशा इसकी आवश्यकता पर प्रश्न चिह्न लगाया जा रहा है। इण्डियन इंस्टीयूट ऑफ मैनेजमेण्ट अहमदाबाद द्वारा जारी परियोजना से सम्बन्धित एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यदि रु4500-5000 के किराए पर कम-से-कम 1,00,000 यात्री रोजाना यात्रा करें, तब जाकर कहीं इस परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ या हानि की गणना की जा सकेगी।

गौरतलब है कि अहमदाबाद से मुम्बई के लिए हवाई यात्रा का टिकट रु2500 में उपलब्ध है। ऐसे में इस बात की पूरी सम्भावना है कि बुलेट ट्रेन की टिकटें सब्सिडाइज्ड दरों पर उपलब्ध होंगी और इससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ेगा। एक किलोमीटर मेट्रो मार्ग के निर्माण में ढाई * सौ करोड़ का खर्च आता है और इस पर अधिकतम 100 किलोमिटर प्रति घण्टे की रफतार वाली ट्रेनें चलती हैं। ऐसे में 320 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफतार वाली ट्रेन के लिए पथ निर्माण का ढाँचा और प्रक्रिया काफी खचींली होगी। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान लागत में कम- से-कम 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है।
भारत, जापान की महँगी तकनीक शिनकानसेन को अपनाएगा। विदित है कि हाई स्पीड रेल निमार्ण की जापानी तकनीक पर होने वाला खर्च स्वर्णिम चतुर्भुज रेल गलियारे के निर्माण पर आने वाले खर्च से 15 गुना अधिक है। इस कारण यह तर्कसंगत नहीं लगता कि रेल के क्षेत्र में इतनी महंगी तकनीक का भारत आयात करे।
यह विचारणीय है कि दुनिया का पाँचों सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होने के बावजूद भारत में कोई भी हाई स्पीड कॉरिडोर नहीं है, जबकि दुनिया के एक दर्जन से अधिक देशों में यह मौजूद है। अतः इस परियोजना क्रियान्वयन की चुनौतियों सन्तोषजनक हैं।
कुछ लोगों द्वारा वह तर्क भी दिया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन के प्रारम्भ करने से पहले भारत को अपने वर्तमान रेलवे ढाँचे को मजबूत करना चाहिए तत्पश्चात् बुलेट ट्रेन के बारे में सोचा जाना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि नई परियोजना से केवल कुछ प्रमुख व्यक्ति ही लाभ उठा सकेंगे जबकि आबादी लाभ नहीं उठा सकेगी।
चुनौतियों का समाधान
मानव जाति का आरम्भ से ही रफतार के प्रति आकर्षण रहा है। परिवहन के सभी माध्यमों में एक-दूसरे को पीछे करने की होड़ मची रहती है और बुलेट ट्रेन का उद्भव रेलवे की इसी होड़ का परिणाम है। आज राष्ट्रों के पास हाई स्पीड नेटवर्क का होना एक ‘स्टेटस सिम्बल’ बन चुका है। इसलिए भारत भी पीछे नहीं रह सकता है।
बुलेट ट्रेन में होने वला निवेश और रेल सरंचनाओं के विकास में होने वाले निवेश को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस निवेश का रेलवे विकल्प नहीं है। बुलेट ट्रेन के लिए अलग कॉरिडोर और बजट बनाया जाना चाहिए।
जापान की हाई स्पीड ट्रेन शिनकानसेन अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है। साथ ही वह बेहतर कार्य संस्कृति से परिपूर्ण होगी, जिसमें जापानी कार्य संस्कृति, समयबद्धता, कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता का सन्देश मौजूद होगा। इससे भारतीय रेल की तस्वीर बदल जाएगी।

भारत के पास बुलेट ट्रेनों के परिचालन की तकनीक मौजूद नहीं थी और न ही भारत के पास इतनी बड़ी पूँजी थी कि वह इस तकनीक में निवेश कर सके। जापान द्वारा सस्ते कर्ज और उसकी शिनकानसेन तकनीक दोनों को प्राप्त कर भारत ने एक पंथ और दो कार्य साधने की कोशिश की है।
चुनौती इस परियोजना पर होने वाले भारी खर्च से समबन्धत है, लेकिन इस नेटवर्क का निर्माण भारत में हुई मेट्रो लाइनों के निमार्ण की तर्ज पर ही किया जाएगा, जिससे लागत को कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के निर्माण हेतु सभी पक्षों की सहमति एवं सहयोग लेने का प्रयास किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
उपर्युक्त तथ्यों, के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में परिवहन के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि यह माना जाता है परिवहन ही किसी देश के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।
अतः भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना का शुभारम्भ एक सरहानीय कदम है किन्तु यह भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि अन्य रेलमार्ग परियोजनाओं के विकास को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि दोनों के समन्वित सहयोग से देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके।
Important Link
- पाठ्यक्रम का सामाजिक आधार: Impact of Modern Societal Issues
- मनोवैज्ञानिक आधार का योगदान और पाठ्यक्रम में भूमिका|Contribution of psychological basis and role in curriculum
- पाठ्यचर्या नियोजन का आधार |basis of curriculum planning
राष्ट्रीय एकता में कौन सी बाधाएं है(What are the obstacles to national unity) - पाठ्यचर्या प्रारुप के प्रमुख घटकों या चरणों का उल्लेख कीजिए।|Mention the major components or stages of curriculum design.
- अधिगमकर्ता के अनुभवों के चयन का निर्धारण किस प्रकार होता है? विवेचना कीजिए।How is a learner’s choice of experiences determined? To discuss.
- विकास की रणनीतियाँ, प्रक्रिया के चरण|Development strategies, stages of the process
Disclaimer: chronobazaar.com is created only for the purpose of education and knowledge. For any queries, disclaimer is requested to kindly contact us. We assure you we will do our best. We do not support piracy. If in any way it violates the law or there is any problem, please mail us on chronobazaar2.0@gmail.com



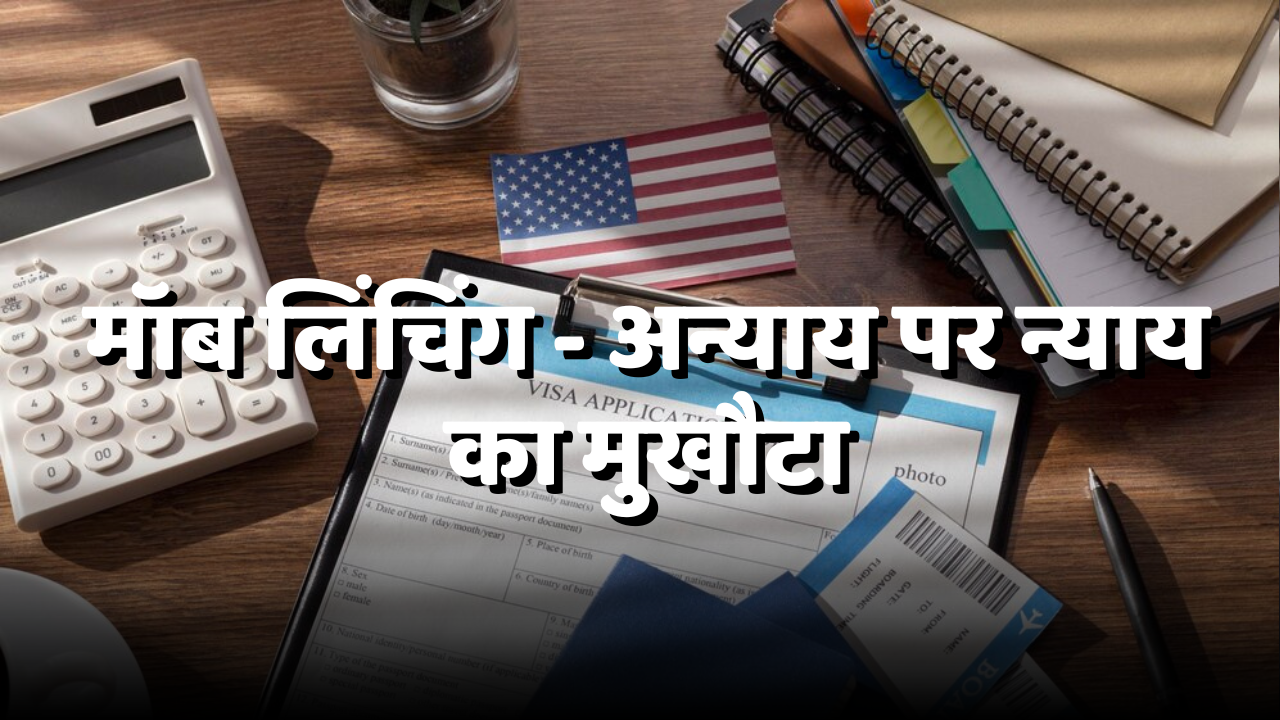

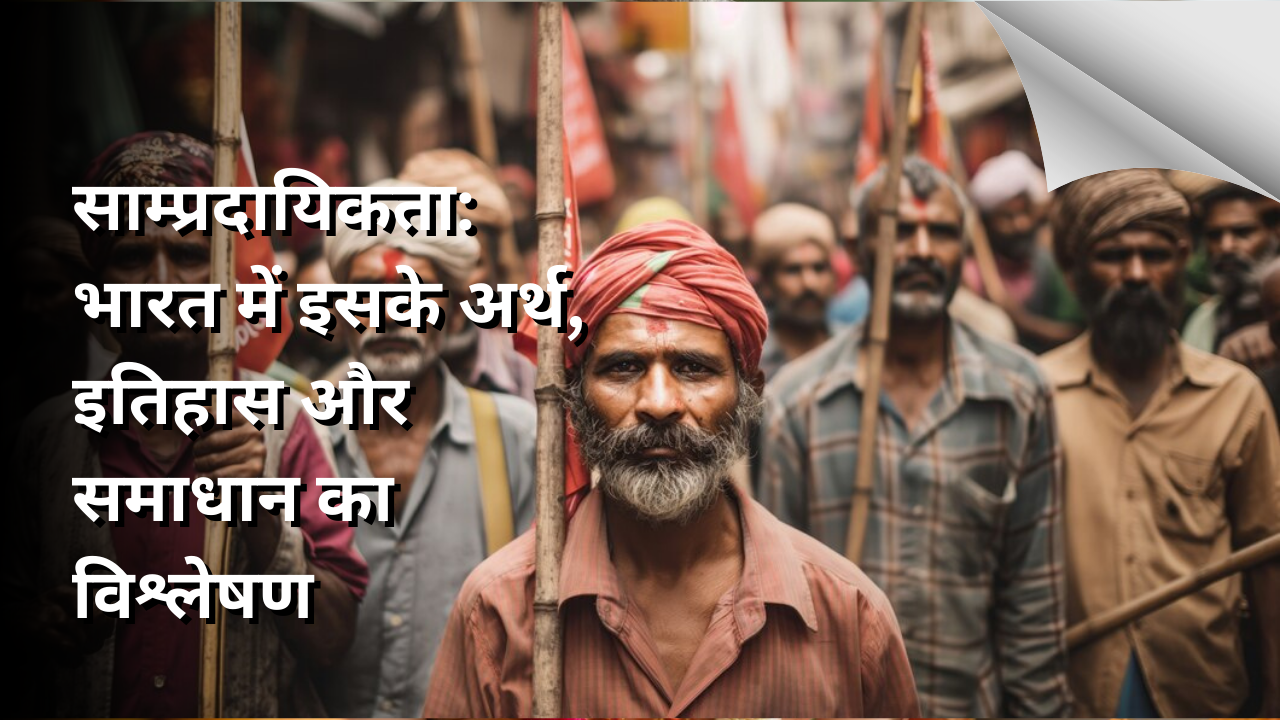



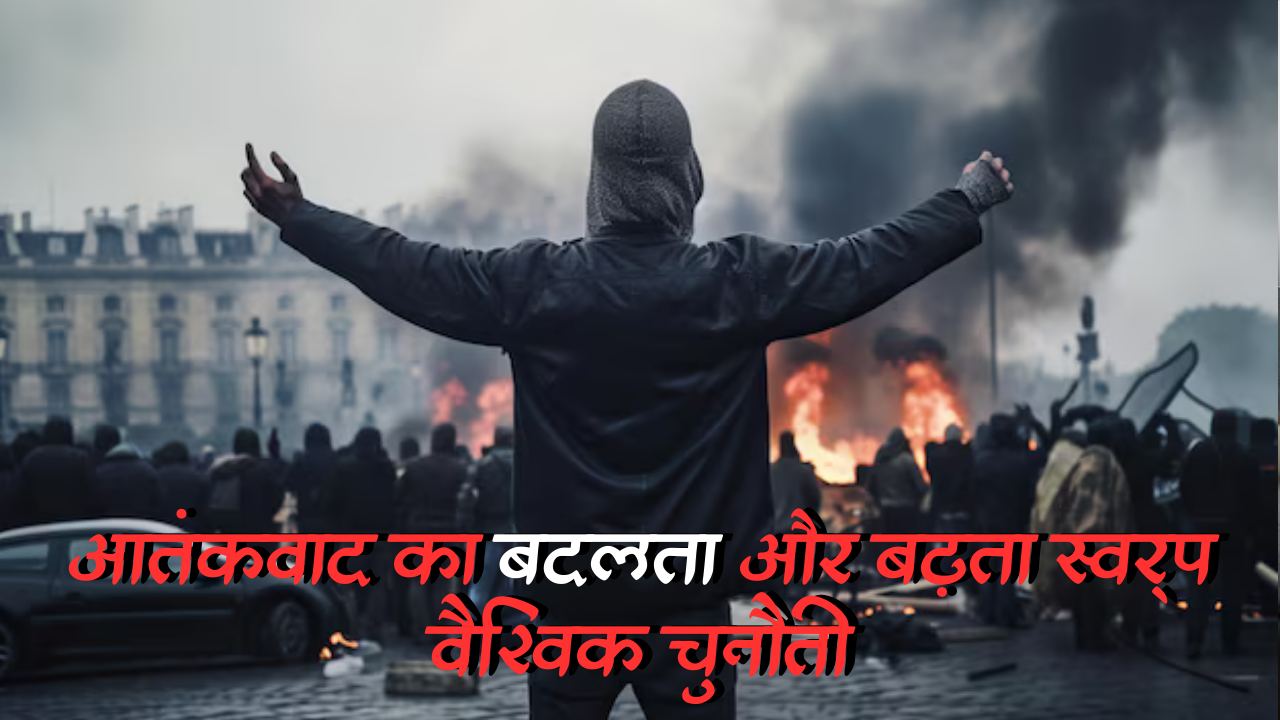
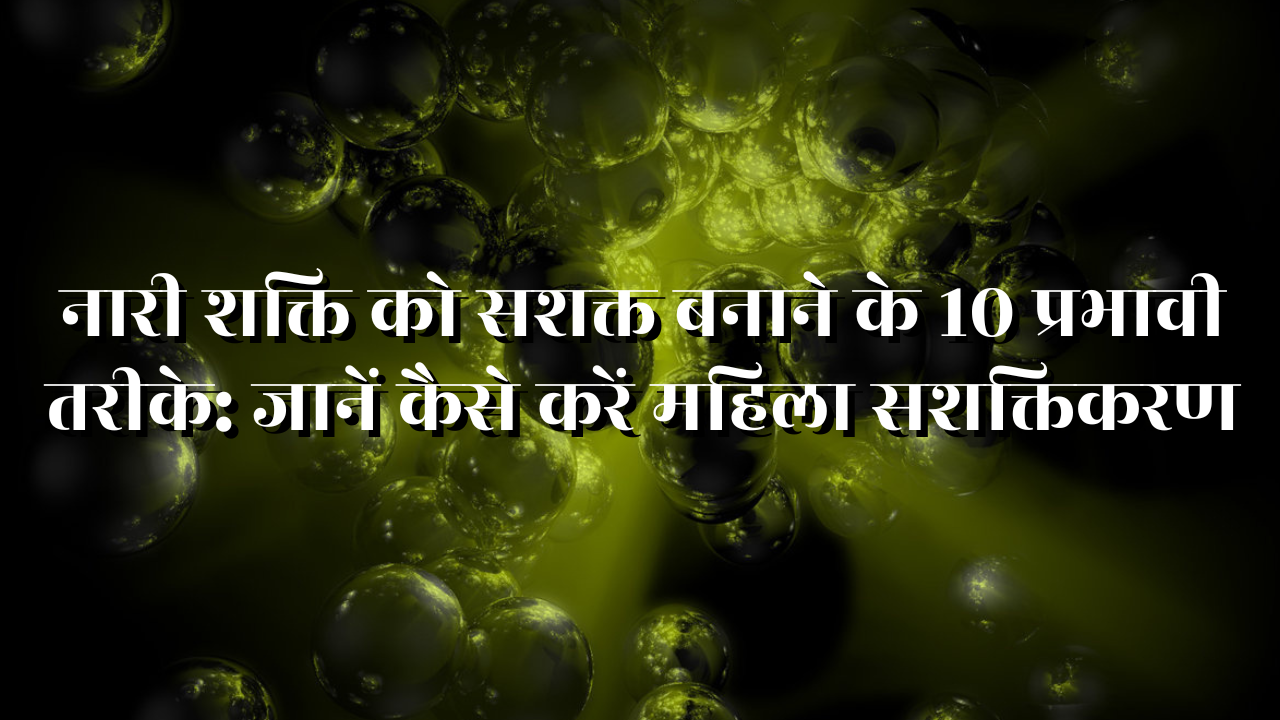
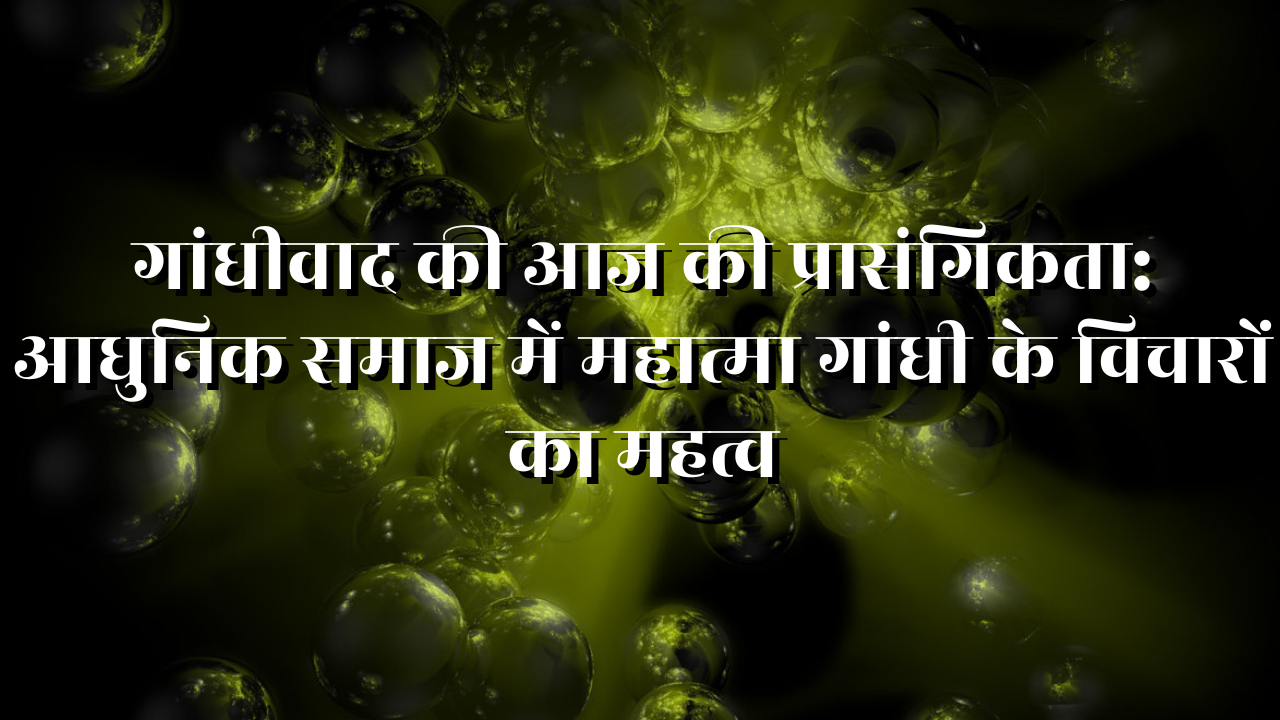

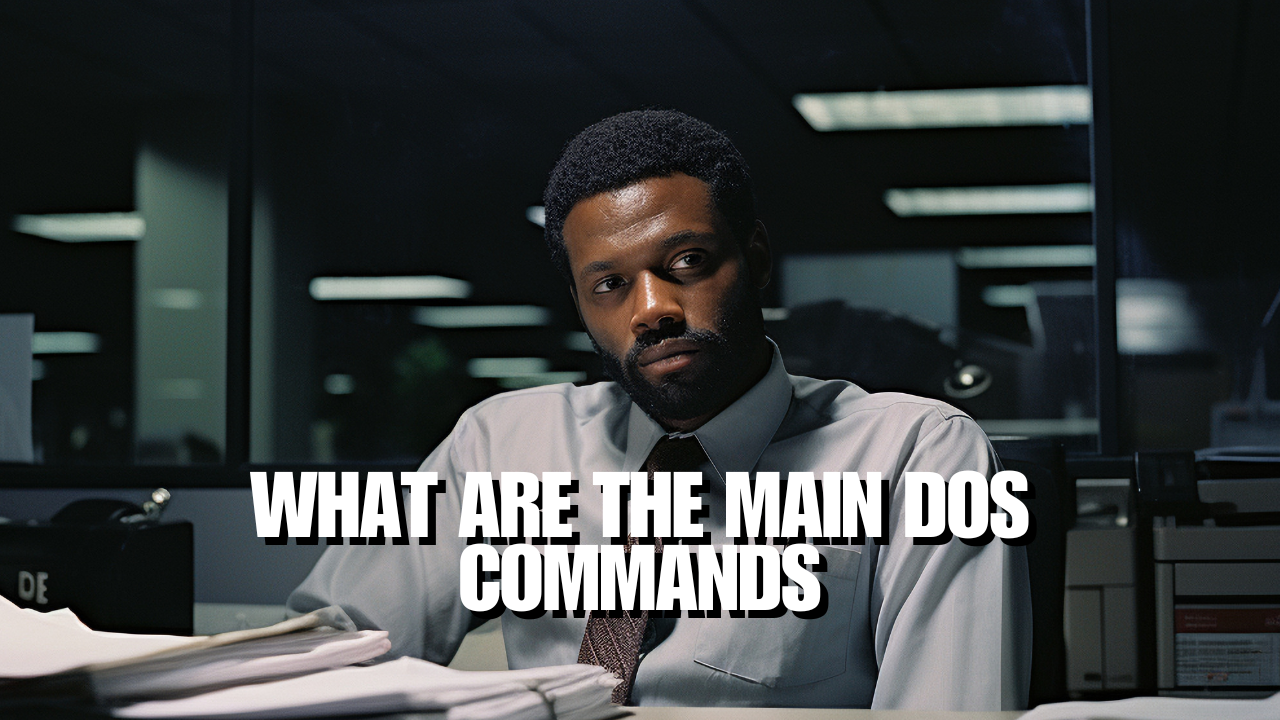
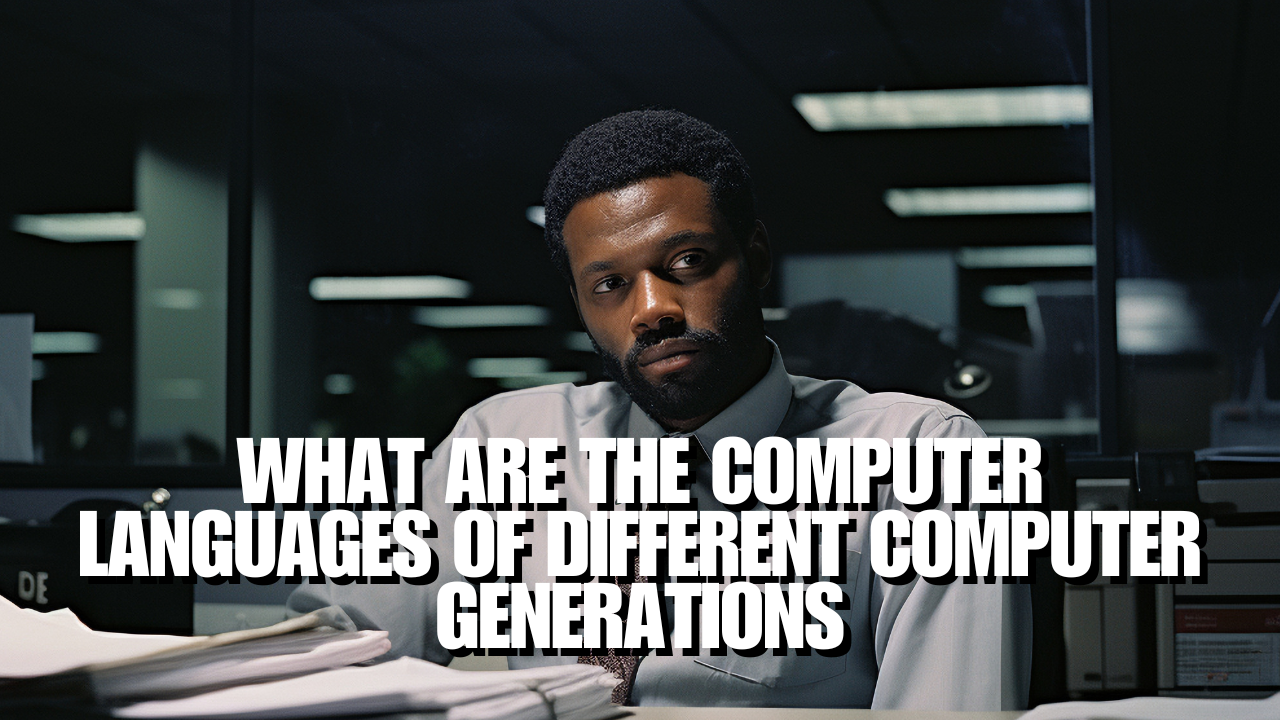

Leave a Reply