तुलसीदास का साहित्यिक योगदान|Literary contribution of Tulsidas
हिन्दी साहित्य के समूचे इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व अप्रतिम हैं। उनकी वाणी एक ऐसे समाधिस्थ चित्त की अभिव्यक्ति है, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, कला का अद्भुत संयोजन है। वह अनास्था के सिंधु में आस्था का समुद्र हैं। तुलसीदास का संपूर्ण साहित्य अतीत के पुनराख्यान से बढ़कर आगत का बोधक व अनागत का दिशासूचक भी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि तुलसीदास का साहित्य भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। इस समूचे साहित्य में लौकिक व आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों का अद्भुत मार्गदर्शन होता है।
तुलसीदास के जीवन संबंधी अधिकांश तथ्यों व घटनाओं पर विवाद है। तुलसीदास का व्यक्तित्व विचित्र विरोधाभासों का समुच्चय है। आर्थिक विपन्नता के कारण उन्हें दर-दर भटकना पड़ा और लक्ष्मी ने उन्हें अंगीकृत भी किया। समाज ने उन्हें तिरस्कृत भी किया और सर्वोच्च सम्मान भी दिया। वह रति क्रीड़ा में आकंत मग्न भी हुए और परम विरागी संत भी हुए।
विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य निर्दिष्ट प्रयोजनों को दो वर्गों में रखा गया है-कवि निष्ठ प्रयोजन व भाव निष्ठ प्रयोजन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन दोनों को स्वीकार किया है। उनकी रचना का एक उद्देश्य स्वांतः सुखाय, प्रबोधात्मक प्रवृत्ति व मोह-भ्रम का निवारण है तो दूसरा जनकल्याण, लोकमंगल और जनमोह का निराकरण है।
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा- 1
स्वान्तस्तमः शांतये-2
भाषाबद्ध करबि मैं सोई।
मोरे मन प्रबोध जेहिं होई ॥
उनकी लोक चिंतन की भावना रामचरितमानस में स्पष्ट है-
मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी तथा रघुनाथ की
कीरति भनिति भूति भलि सोई।
सुरसरि सम सब कहैं हित होई ॥
तुलसीदास का विश्वास है कि सच्ची कविता वही है जो कवि के हृदय से निकलकर पाठक हृदय को आह्लादित कर दे। वस्तुतः काव्यात्मक श्रेष्ठता की पहली कसौटी समाज है। गोस्वामी जी में लोकमंगल और काव्यकौशल का चरम परिपाक मिलता है। तुलसीदास जी राम जैसे लोकनायक का चरित्र वर्णित कर देने मात्र से सम्मान की पराकाष्ठा पर स्थापित नहीं हुए हैं। राम का जीवन भले ही काव्य की प्रेरणा हो, किंतु प्रत्येक रामकथा का कवि तुलसी नहीं बन सकता, जैसे न केशव बन सके और न मैथिलीशरण गुप्त।
सूर ने ऐसे ‘सागर’ का निर्माण किया जिसकी प्रेरणा से परवर्ती कवियों द्वारा प्रभूत कृष्ण काव्य लिखे गए और तुलसी का ‘मानस’ इतना अथाह बना कि उसके पश्चात् रामकाव्य प्रणयन की परंपरा ही अवरुद्ध सी हो गयी। तुलसीदास जी में व्यापक प्रतिभा और अप्रतिम काव्यदृष्टि विद्यमान थी। उनमें शक्ति, निपुणता और अभ्यास का सुंदरतम सामंजस्य है और भाव तथा कलापक्ष संतुलित है यद्यपि वे भाव पक्ष को प्रधानता हैं और कला का गौण मानते हैं। उनके लिए भाव साध्य है और कला साधन।
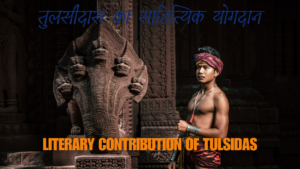
गोस्वामी जी के समय तक संस्कृत अलंकार प्रधान चमत्कारों से बोझिल हो गयी थी और उसका दायरा उच्च वर्ग के समाज तक सिकुड़ गया था। विडंबना यह थी कि भाषा में भी आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी थी।
हिंदी कविता, छंद-वैविध्य और अलंकार प्राचुर्य की बोझिलता से क्लिष्ट होती जा रही थी। ऐसे में गोस्वामी जी ने आचार्य प्रदर्शन की भावना से बच कर बड़े विनम्र शब्दों में ‘कवित विवेक’ के प्रति अपना अज्ञान व्यक्त किया है-
कवि न होउँ नहिं वचन प्रवीनू।
सकल कला सब विद्या हीनू ॥
यहाँ पर तुलसीदास जी तत्कालीन प्रचलित संकीर्ण साहित्यिक मान्यताओं को सिरे से नकार एक समर्पित लोकचिंतक की भूमिका का निर्वाह करते हैं जो मानव मात्र के लिए अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करता है।
तुलसीदास जी हिंदी के ऐसे कवि हैं, जिन्होंने प्रबन्धकाव्य एवं मुक्तक काव्य दोनों प्रकार के ग्रंथों की रचना की और दोनों ही काव्यरूपों के प्रणयन में विशेषज्ञता प्राप्त की। मुक्तक काव्य में जहाँ छंदों में पूर्वा-पर संबंध का अभाव होता है और प्रत्येक छंद अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र हाता है, वही प्रबंध काव्य में एक सानुबंध कथा होती है। संपूर्ण घटनाक्रम कार्य कारण संबंध से परस्पर पूर्वापर संबंधों का निर्वाह करते हुए जुड़ा रहता है।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में एक उच्चकोटि का प्रबंध लिखा तो दूसरी ओर विनयपत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, श्रीकृष्णगीतावली जैसे उत्कृष्ट मुक्तक काव्य भी उन्होंने लिखे हैं।
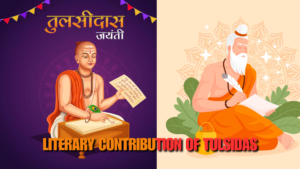
आचार्य शुक्ल ने प्रबंध सौष्ठव के लिए तीन मानक स्थापित किए हैं- 1. संबंध निर्वाह, 2. कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, 3. दृश्यों की स्थानागत विशेषता|
रामचरित मानस में इन तीनों तत्वों का सफल निर्वाह दिखाई पड़ता है। रामचरित मानवस की कथा आदि से अंत तक अक्षुण्ण बनी रहती है। वह कहीं से भी विश्रृंखलित नहीं होती है। इस महाकाव्य में राम के जन्म से लेकर राज्यारोहण तक की गतिविधियों सात काण्डों में विभक्त की गयी हैं- बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्धिाकांड, सुंदरकाण्ड, लंकाकाण्ड, उत्तरकाण्ड।
पूरे रामचरित मानस में कथा कहीं भी बोझिल नहीं होती साथ ही कहीं भी वह असामान्य प्रतीत नहीं होती है।
रामचरित मानस हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है, जिसकी रचना 1574 ई. में हुई थी। यह काव्यग्रंथ अपनी प्रबंध कल्पना, उत्कृष्ट रचना कौशल, प्रभावोत्पादक भाव व्यंजना,प्रसंगानुकूल सरस भाषा, भावानुकूल छंद विधान की दृष्टि से उच्चतम माना गया है।
इसके कथानक में महाकाव्योचित्त गरिमा विद्यमान है, जो प्रख्यात रामकथा पर आधृत है। इसमें प्रकृति के विविध रूपों की झाँकी है, सभी ऋतुओं का वर्णन है, साथ ही सभी प्राकृतिक रमणीय व भयानक रूपों का चित्रण भी है।
उत्तरकाण्ड में कलियुग का वर्णन करते हुए उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का विशद चित्रण किया है-
बरन धर्म नहिं आश्रम चारी। श्रुति विरोधरत सब नर-नारी।
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासना। कोऊ नहिं मान निगम अनुशासन ।
मारग सोइजा कहुँ जोई भावा। पंडित सोई जो गाल बजाया।
मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कहूँ संत कहइ सब कोई।
सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी।
रामराज्य की जो परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की है वह आदर्श राजव्यवस्था का प्रारूप है।
भाषा एवं रस निरूपण की दृष्टि से भी यह एक सफल महाकाव्य है। इसमें सभी रसों की योजना की गयी है। रामचरित मानस में स्वान्तः सुखाय व लोकमंगल का अपूर्व सम्मिलिन है। इसका कलापक्ष भी बेजोड़ है। इसकी अलंकार योजना, छंद विधान एवं भाषासौष्ठव भी महाकाव्योचित्त है। सारांशतः कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी में प्रबंध काव्य की अद्भुत प्रतिभा विद्यमान थी।
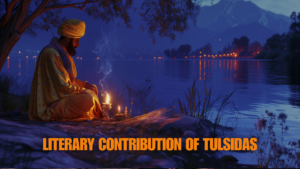
तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य में ‘मर्यादावाद’ की स्थापना की। उनकी मान्यता थी कि लोकमर्यादा का पालन करने से ही समाज कल्याण संभव है। उनके श्रृंगार वर्णन में भी मर्यादित प्रवृत्ति व्याप्त है, कहीं भी अश्लीलता का नामोनिशान नहीं है। पुष्पवाटिका में राम और सीता के प्रथम मिलन के प्रसंगों में शृंगार का मर्यादापूर्ण, आलंबन अद्भुत है।
कंकन किंकिनि नुपूर धुन सुनि,
कहत लखन सन राम मनहिं गुन
मानहु मदन दुन्दुभी दीन्हौं,
मनसा विश्व विजय करि लीन्हौं ।
रामचरित मानस में सर्वत्र मर्यादा पालन पर जोर दिया गया है। उनके मर्यादावाद में न तो एकांगिता है और न ही धार्मिक मजहबीपन। मानस धर्म की भावभूमि पर रचित साहित्यिक ग्रंथ है, जिसमें भक्ति को मर्यादा के साथ स्थापित कर नई पहल की गयी है। भक्ति करने वाला ‘अन्त्यज’ भी सबसे अधिक वंदनीय है। तुलसीदास के श्रीराम ने निषाद राज को अपना मित्र बनाया और शबरी के जूठे बेर खाकर इसकी पुष्टि कर दी।
तुलसीदास जी के शिल्प पक्ष पर अब तक काफी विचार किया जा चुका है। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल की समीक्षा समीचीन प्रतीत होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को संतोष है कि तुलसीदास जी ने हिंदी के अन्य कवियों की भाँति ‘वस्तु-परिगणन-शैली’ का उपयोग नहीं किया है। यही नहीं, उन्होंने भिन्न-भिन्न व्यापारों में तत्पर मनुष्यों की विशिष्ट मुद्राओं का भी बड़ा ही स्वाभाविक और बिम्बात्मक चित्रण किया है। मारीच के पीछे शर-संधान किए हुए राम और राम की प्रतीक्षा में माथे पर हाथ रखकर दूर देखती हुए शबरी की मुद्राओं का उदाहरण देकर उन्होंने अपनी बात की पुष्टि की है।
तुलसीदास जी ने अलंकार विधान में उन्हीं अलंकारों को महत्त्व दिया है, जो भावों को उत्कर्ष स्वरूप देने तथा वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया के अनुभव को तीव्र करने में सहायक हैं। उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पर्यायोक्ति, विभावना, असंगति, व्यतिरेक, मीलित उन्मीलित, संदेह आदि अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विस्तृत व्याख्या के साथ प्रमाणित किया है कि गोस्वामी जी ने रूप, गुण, क्रिया व भावों को उत्कर्ष देने के लिए इनका प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल ने लक्ष्यित किया है कि तुलसी की भाषा चलती हुई और मुहावरेदार है। उनकी वाक्य रचना निर्दोष है। उन्होंने पादपूर्ति के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी महत्त्व के साक्षात्कार के लघु प्रयत्न के रूप में ‘गोस्वामी तुलसीदास’ नामक चर्चित रचना की है।
तुलसी ने अपने गीतों में अलंकारिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की भाषाओं का भावानुकूल प्रयोग किया है। कहीं भाषा सामासिक है तो कहीं सरल सहज व व्यास प्रधान। अपने प्रगीतकाव्य में तुलसी ने पारंपरिक ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। शब्द शक्तियों के उचित प्रयोग से भावों की अभिव्यक्ति अधिक मार्मिक एवं व्यंग्यपूर्ण हो गयी है।
तुलसी ने अपने समय में प्रचलित काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज में रचना करके साहित्यिक समन्वय का अनूठा प्रयास किया। अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों दोहा-चौपाई, कवित्त, सवैया पद, बरवै, आदि में रचनाएँ कर कथा शैली व स्स्रोत शैली का संयोजन किया।
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि तुलसी अपने समय के महान समन्वयवादी थे। वे आत्ममुग्धता की प्रवृत्ति से आजीवन अछूते रहे। सदैव स्वान्तः सुखाय की पृष्ठभूमि में जननेता की भूमिका का निर्वाह करते रहे।
खंडन-मंडन की प्रवृत्ति से परे रहकर अखण्डता को नकार कर तुलसी ने समन्वयवादी दृष्टि का परिचय दिया। समाज और साहित्य जगत में व्याप्त कटुता, विषमता, विद्वेष और वैमनस्य को दूर कर पारस्परिक स्नेह, सहानुभूति, सौहार्द्र-समता का वातावरण स्तजित कर साहित्य को अनूठी गरिमा प्रदान की। वे सच्चे अर्थों में महान सुधारक, समन्वयकर्त्ता, लोकनायक और साहित्य की आत्मा को धारित करने वाले जन कवि थे।
Important Link
- पाठ्यक्रम का सामाजिक आधार: Impact of Modern Societal Issues
- मनोवैज्ञानिक आधार का योगदान और पाठ्यक्रम में भूमिका|Contribution of psychological basis and role in curriculum
- पाठ्यचर्या नियोजन का आधार |basis of curriculum planning
राष्ट्रीय एकता में कौन सी बाधाएं है(What are the obstacles to national unity) - पाठ्यचर्या प्रारुप के प्रमुख घटकों या चरणों का उल्लेख कीजिए।|Mention the major components or stages of curriculum design.
- अधिगमकर्ता के अनुभवों के चयन का निर्धारण किस प्रकार होता है? विवेचना कीजिए।How is a learner’s choice of experiences determined? To discuss.
- विकास की रणनीतियाँ, प्रक्रिया के चरण|Development strategies, stages of the process
Disclaimer: chronobazaar.com is created only for the purpose of education and knowledge. For any queries, disclaimer is requested to kindly contact us. We assure you we will do our best. We do not support piracy. If in any way it violates the law or there is any problem, please mail us on chronobazaar2.0@gmail.com

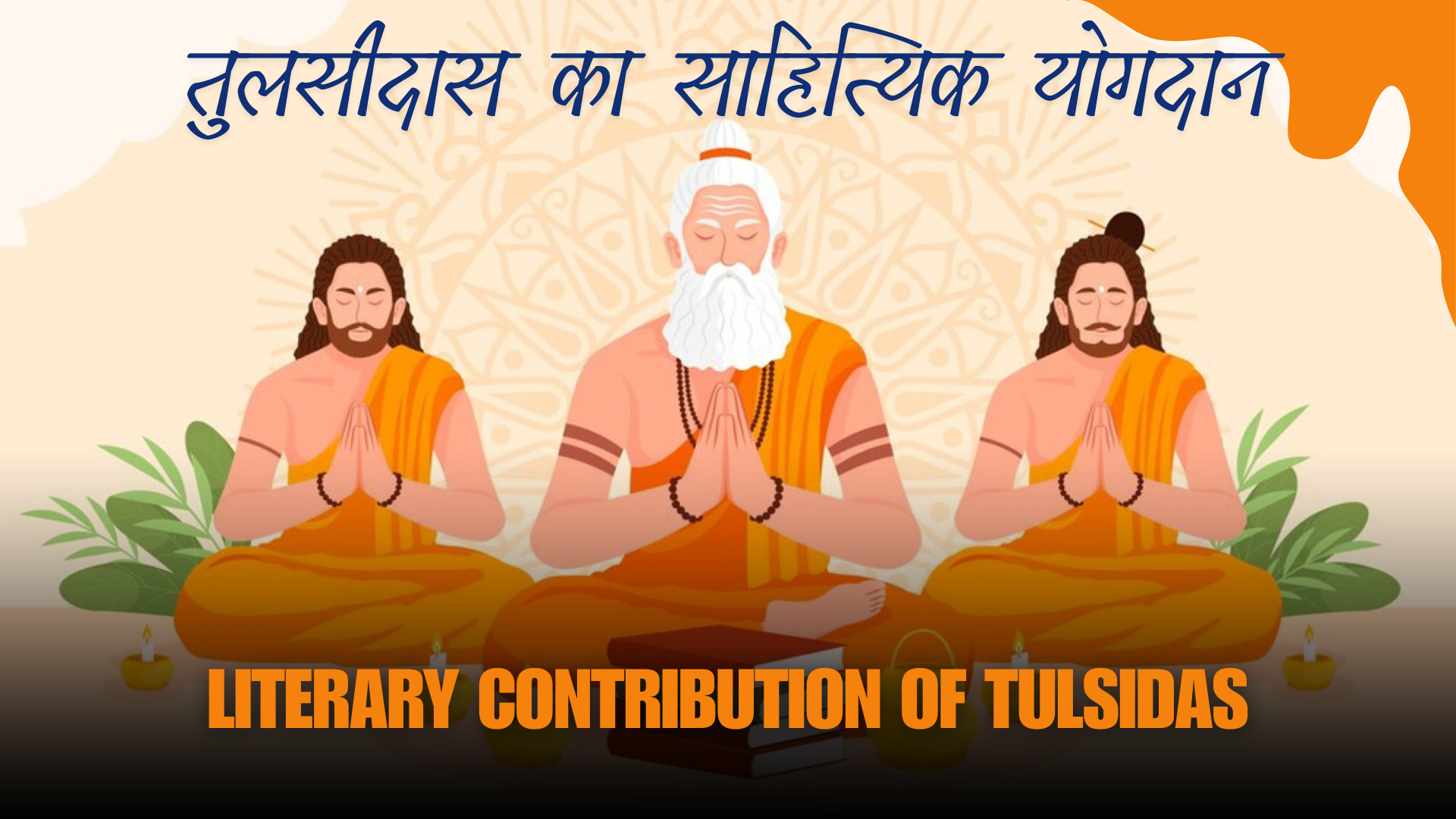

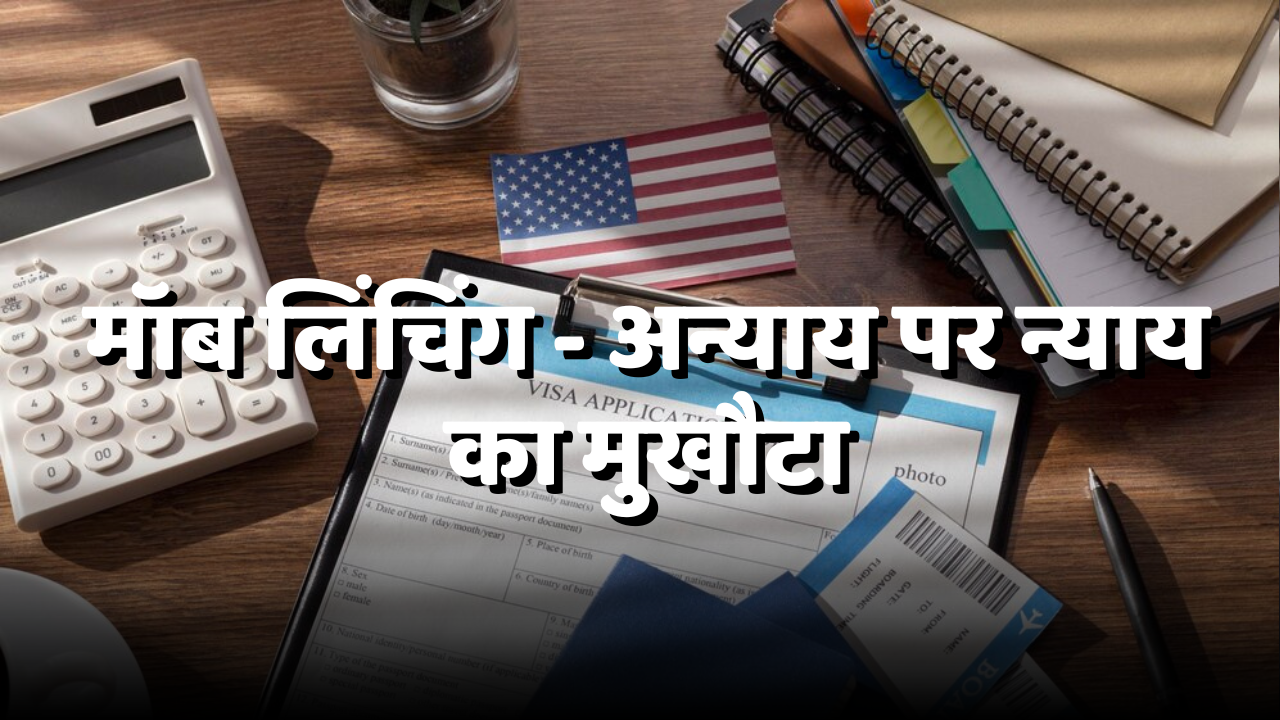

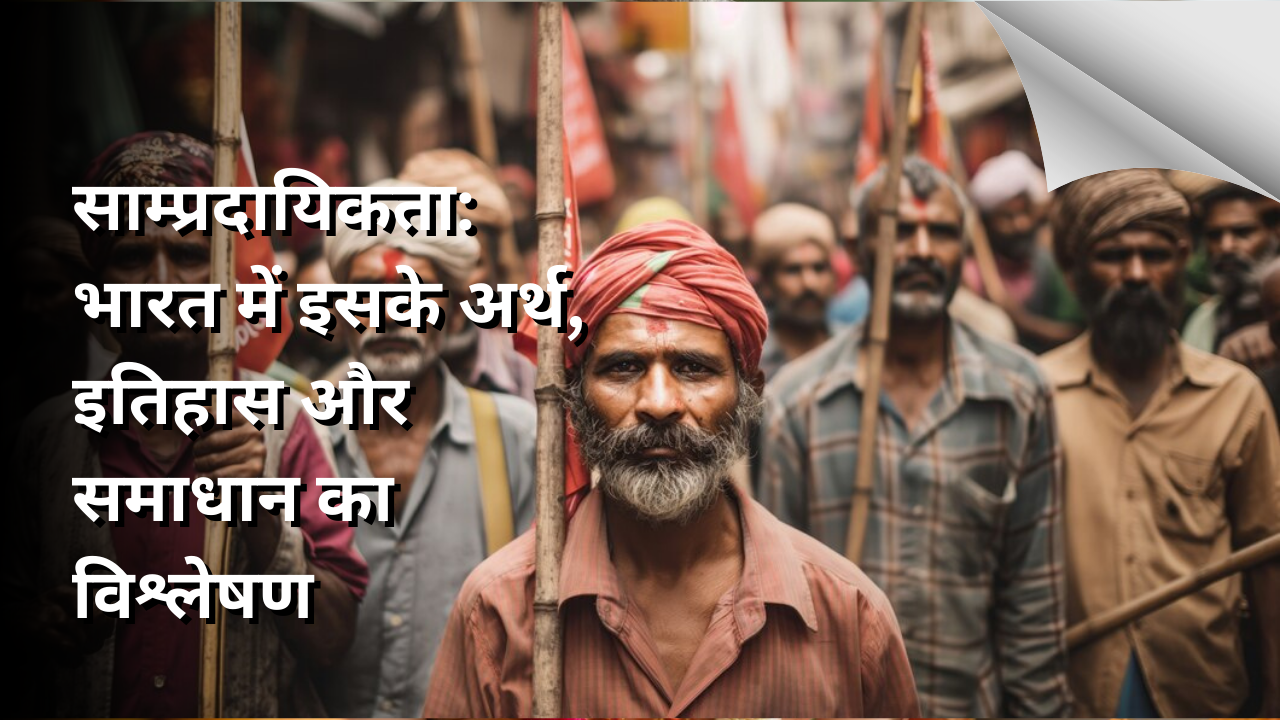



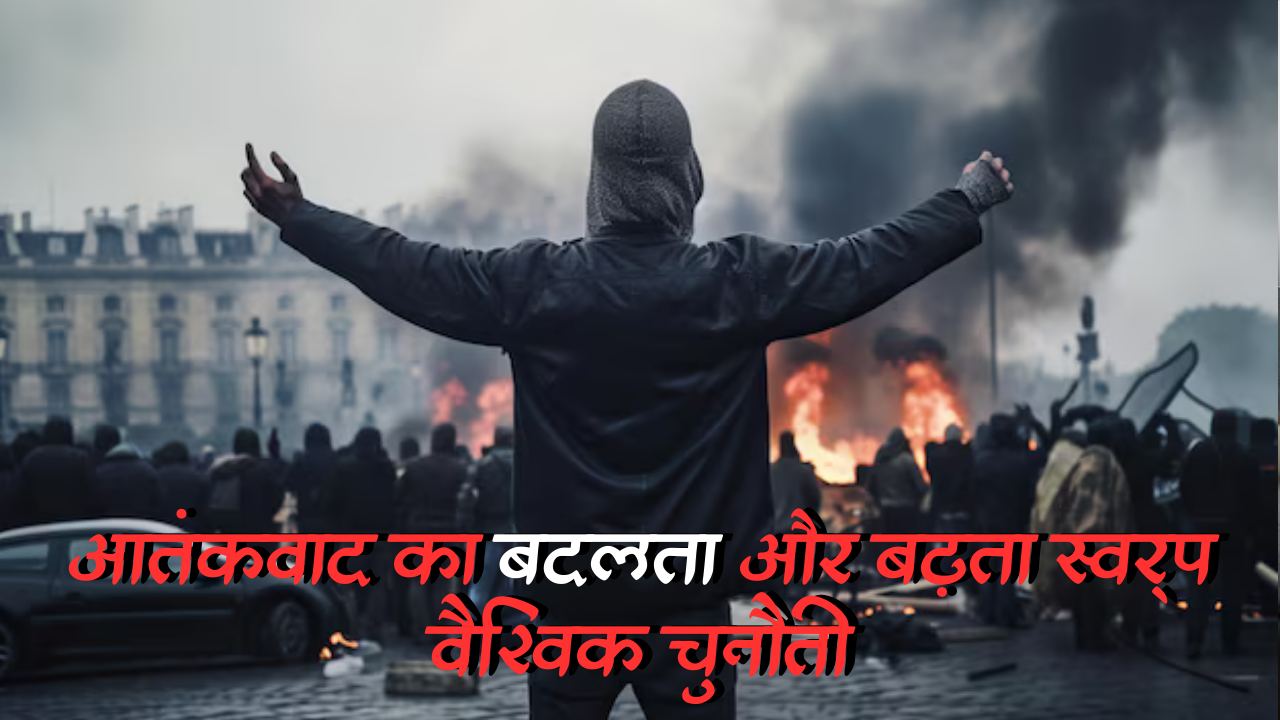
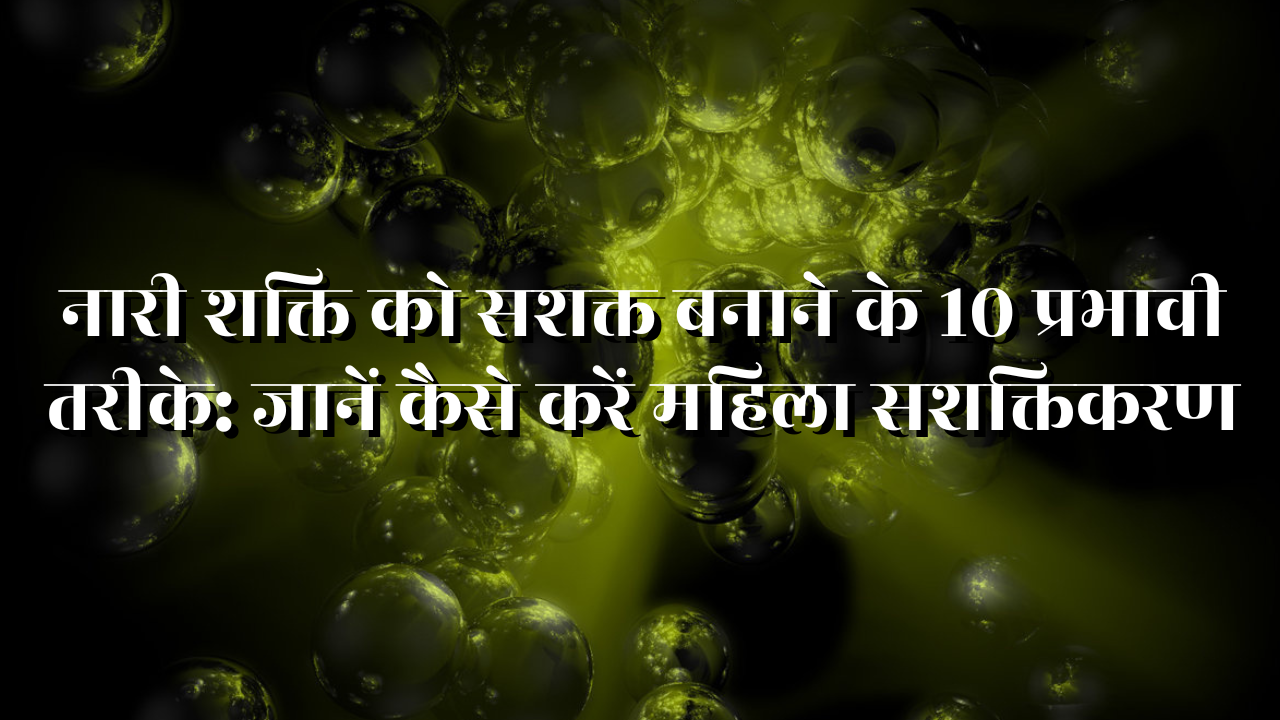
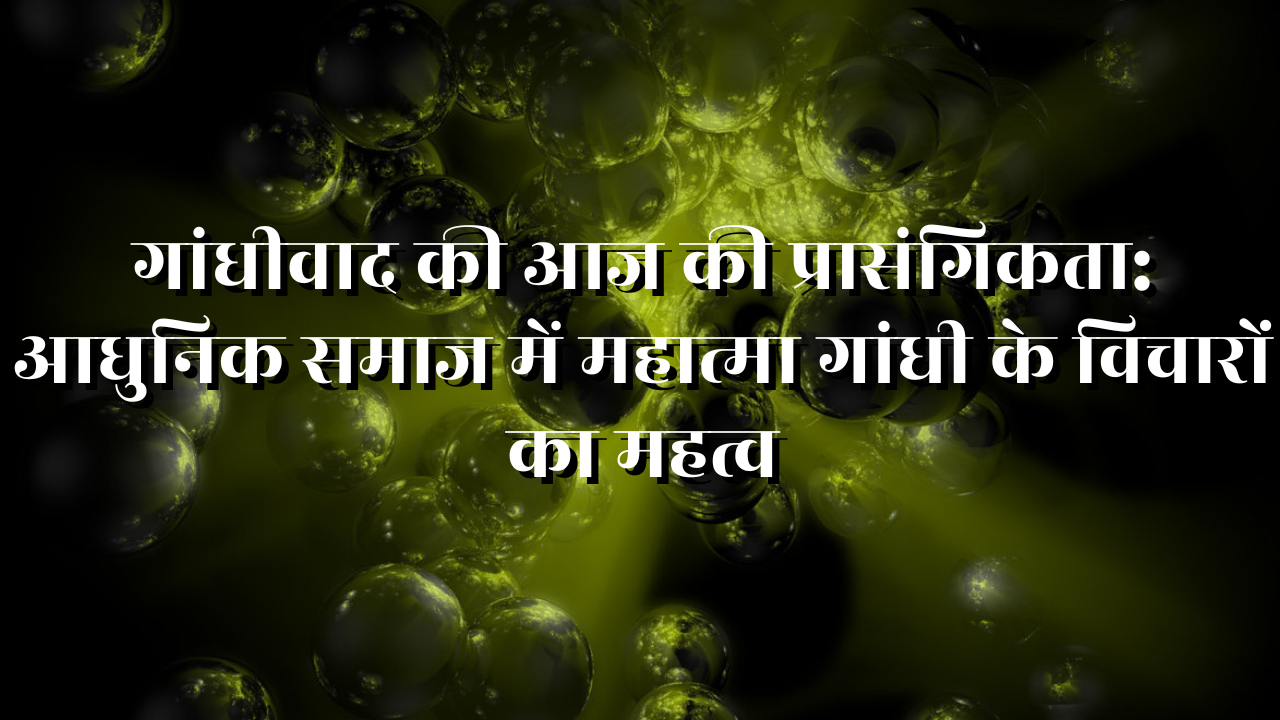

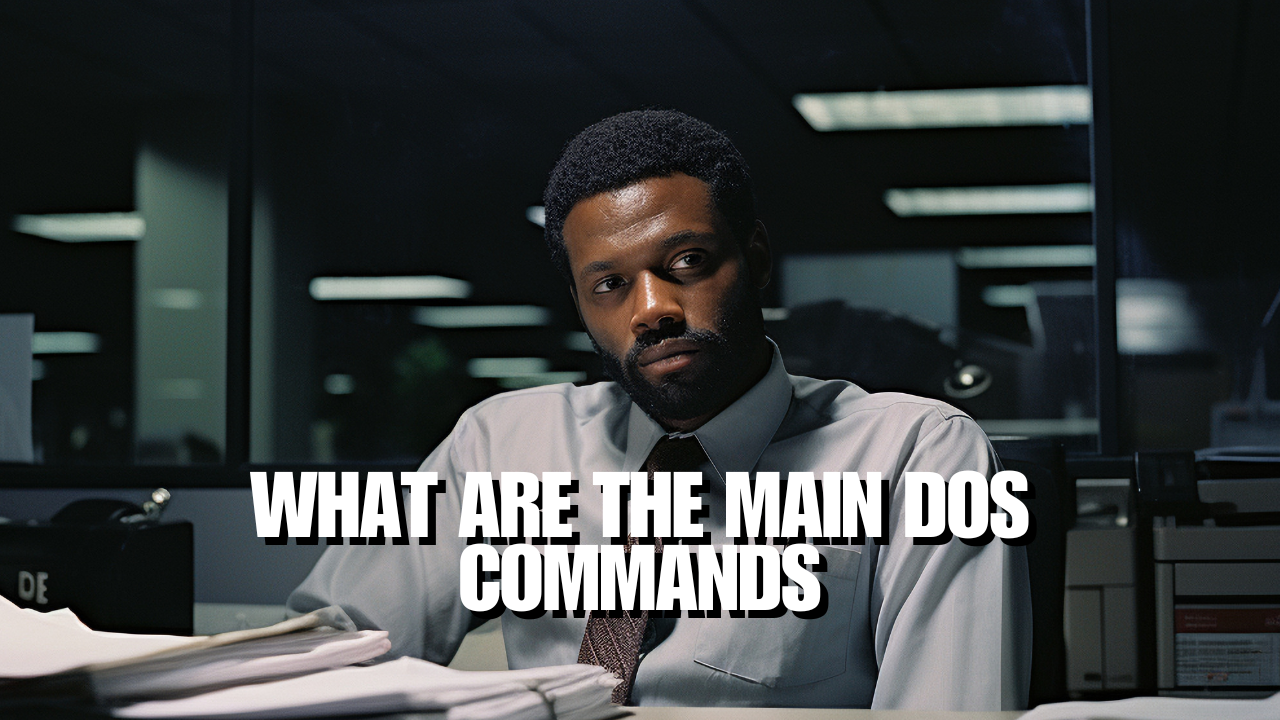
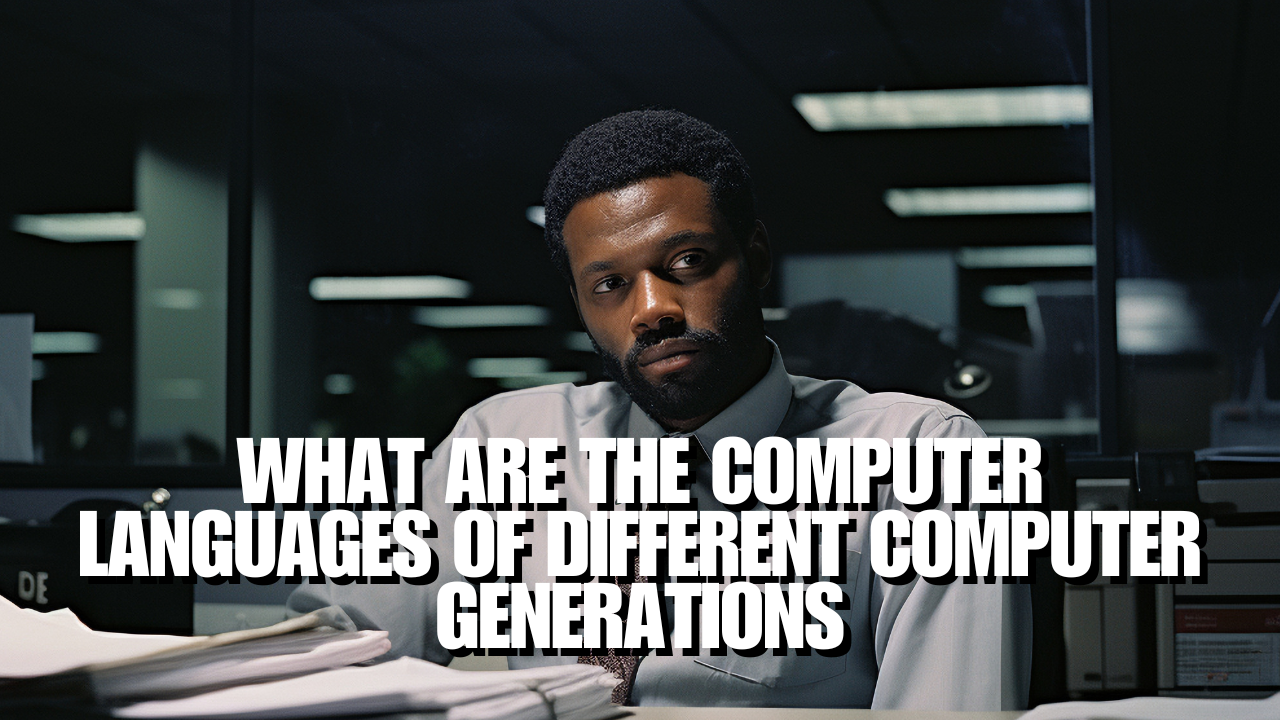

Leave a Reply