कुंभ पर्व : मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत|Kumbh Festival: Intangible Cultural Heritage of Humanity
बहते-बहते सागर में समा जाना तो नन्दियों की नियति है, लेकिन स्वयं सागर को नदियों में समाहित होते देखना चमत्कार ही है। यह चमत्कार साकार होता है कुंभ पर्व के दौरान, जब अथाह जनसिंधु त्रिविधि ताप-पापनाशिनी नदियों की गोद में कुछ पलों की ही पनाह पाने को आतुर दिखता है।
भारतीय परंपरा में तर्क पहले आया, फिर प्रतितर्क और फिर विज्ञान। भारतीय दर्शन का विकास किसी आस्था से नहीं हुआ। उपनिषद दर्शन के समय हीगल, मार्क्स तो दूर पाइथागोरस, सुकरात और अरस्तू का भी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन भारत में सृष्टि रचना के आदिकरण, आदिस्रोत पर बहस जारी थी। मृत्यु की स्वाभाविकता के बावजूद अमरत्व पर बहस जारी थी। मृत्यु की स्वाभाविकता के बावजूद अमरत्व की चाह थी। सुख-दुःख के मनोविज्ञान तथा आनंद के स्त्रोत की खोज जारी थी। ऋषियों द्वारा सौरमंडल के ग्रहों, राशियों की गति के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। गति से ही समय की सत्ता है और समय के विश्लेषण से ही निकला है-कुंभ पर्व।
कुंभ शब्द का उल्लेख वेदों में मिलता है। ऋग्वेद के दशम् मंडल एवं यजुर्वेद व अथर्ववेद में कुंभ शब्द समस्त संसारवादियों के लिए शुभ कर्मों के अनुष्ठान हेतु आता है। समुद्र मंथनजन्य अमृत कुंभ से संबद्ध होने के कारण कुंभ शब्द ‘कुंभ पर्व’ के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
कुंभ शब्द की व्युत्पत्ति 6 प्रकार से की गई है –
(i) ‘कुं पृथ्वी उम्भयपति पुरयाति’ मंगलेन ज्ञानामृतेन वा’ अर्थात जो समस्त पृथ्वी को मंगल ज्ञान से पूर्ण कर दे।
(ii) ‘कुलिग्त उम्भतिः’ अर्थात् जो पर्व संसार के अरिष्ट और पापों को दूर कर दे।
(iii) ‘कुः पृथ्वी उभ्यते अनुग्रह्यते आच्छादते आनंदेन पुण्येन वा’ अर्थात् जिस पर्व के द्वारा पृथ्वी को आनंद व पुण्य से ढक दिया जाए।
(iv) ‘कुः पृथ्वी उभ्यते लह्वी क्रियते प्रक्षालनेन येन’ अर्थात् पृथ्वी पर पापों को धोकर जब उसे हल्का बना दिया, ऐसा पर्व-कुंभ।
(v) ‘कुः पृथ्वी भावयति दीपयति’ अर्थात् जो पर्व पृथ्वी को सुशोभित कर दे, दीप्त कर दे, उसके तेज को बढ़ा दे।
(vi) ‘कुं सुखं ब्रह्म तद उभ्यति प्रयच्छतीति कुंभ’ अर्थात् सुख स्वरूप परम ब्रह्म के अनुभव को प्रदान करने वाले संत समागम का नाम कुंभ है।
कुंभ पर्व चार स्थानों (प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन) पर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक स्थान पर इसके आयोजन का समय, ग्रहों की स्थिति के अनुसार तय किया जाता है।

पौराणिक आख्यानों के अनुसार, ऋषि दुर्वासां के अभिशाप के कारण निर्बल हो चुके देवताओं को असुरों ने पराजित कर दिया था। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने हेतु देवताओं ने भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार, समुद्र मंथन कर अमृत निकालने हेतु असुरों से संधि की। मंथन हेतु मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन द्वारा क्षीर सागर से 14 रत्न निकले, जिनमें कालकूट विष, पुष्पक विमान्, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सरा रंभा, कौस्तुभ मणि, बाल चंद्रमा, कुंडल धनुष, शारंग धनुष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, माँ लक्ष्मी, विश्वकर्मा तथा अमृत कुंभ शामिल हैं।
अमृत कुंभ निकलते ही देवताओं और असुरों में इस पर अधिकार को लेकर युद्ध शुरू हो गया, जो कि 12 दिनों तक चला। इसी दौरान पृथ्वी के चार स्थानों (प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक) पर अमृत कुंभ से अमृत की कुछ बूँदे गिरी थीं। इसलिए इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
एक अन्य मान्यता के अनुसार, आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले की शुरूआत की थी। कुछ विद्वान गुप्तकाल में इसके सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रामाणिक तथ्य सम्राट हर्षवर्धन के समय से प्राप्त होते हैं। ह्वेनसांग ने भी अपने विवरण में कुंभ मेले का उल्लेख किया है।
4-9 दिसंबर, 2017 के मध्य जेजू (दक्षिण कोरिया) में यूनेस्को (UNESCO) की ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु अंतरसरकारी समिति का 12वाँ सत्र’ आयोजित किया गया। इसमें ‘मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ सूची में 33 नए तत्वों (Elements) को शामिल किया गया। इसमें भारत में आयोजित होने वाले ‘कुंभ मेला’ को शामिल किया गया है। कुंभ मेला भारत की 13वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है।

विरासत सिर्फ स्मारकों या कला वस्तुओं के संग्रहण तक ही सीमित नहीं होती वरन् इसमें उन परंपराओं एवं प्रभावी विचारों को भी शामिल किया जाता है, जो पूर्वजों से प्राप्त होते हैं और अगली पीढ़ी को स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे मौखिक रूप से चल रही परंपराएँ, कला-प्रदर्शन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और परंपरागत शिल्प कला। यही अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है।
कुंभ मेले में सब कुछ श्रद्धावश ही है या फिर इसके पार्श्व में कोई वैज्ञानिक आधार भी है? सौरमंडल के विशिष्ट ग्रहों के विशेष राशियों में प्रवेश करने से बना खगोलीय संयोग इस पर्व का आधार है। ज्योतिशास्त्र के अनुसार, सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि की विशेष युतियों में कुछ विशेष किस्म की खगोलीय ऊर्जाएँ पृथ्वी पर चुनिंदा स्थानों पर स्थित जल भंडारों को प्रभावित करती
हैं और यह जल, मनुष्य के स्वास्थ्य व कार्मिक ऊर्जाओं को बल देता है, पुष्ट बनाता है।

इन दिनों क्षेत्र विशेष का वातावरण दिव्य, अद्भुत तरंगों व स्पंदनों से भर जाता है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। यह माँ गंगा की अद्भुत महिमा है, जो भारतीय संस्कृति की महानता का दर्शन कराती है। गंगा जली में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने और इसमें कुछ विशिष्ट विषाणुओं (बैक्टीरियोफेज) के मौजूद होने से यह अत्यधिक विशिष्ट है। जापानी वैज्ञानिक मसारू इमेटो ने गंगा जल पर गहन शोध में पाया कि जल में अत्यंत विशेष प्रकार की संरचनाएँ निर्मित होती हैं, जिनका आधार वहाँ का वातावरण, कॉस्मिक ऊर्जाएँ और वहाँ स्थित भावनाएँ होती हैं। जल के यह विशेष क्रिस्टल मानव ऊर्जाओं को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जल के ये क्रिस्टल शरीर को बनाने और बिगाड़ने में बड़ा योगदान करते हैं। ऋषियों ने लाखों वर्ष पूर्व ही इस सत्य को जान लिया था और विशेष कॉस्मिक परिस्थितियों का लाभ, आने वाली पीढ़ियों को कैसे दिया जाए, इसका तरीका भी उन्होंने ईजाद कर लिया था। वस्तुतः कुंभ पर्व इसी प्रकार की खोज का नतीजा है, जो मानव मात्र के लिए प्रत्येक लिहाज से कल्याणकारी है।
पूर्णता प्राप्त करना मानव का लक्ष्य है। पूर्णता से तात्पर्य है, समग्र जीवन के साथ एकता, एक टुकड़े के रूप में होते हुए अपने समूचे रूप का ध्यान करके अपने छोटेपन से मुक्ति। इसी पूर्णताकी अभिव्यक्ति है-पूर्ण कुंभ। पुराणों में अमृत मंथन की कथा उल्लिखित है। मंथन के पश्चात् अमृत कलश उद्भूत होता है। अमृत की चाह देवता, असुरों सबको है। यह अमृत वस्तुतः कोई द्रव पदार्थ नहीं है, यह मृत न होने का जीवन की आकांक्षा से पूर्ण होने का भाव है। देवता अमर हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि उनमें जीवन की अक्षय भावना है। चारों महाकुंभ उस अमृत भाव को प्राप्त करने के पर्व हैं।
कुंभ अर्थात् घड़े को मानव शरीर का प्रतीक माना गया है, क्योंकि शरीर मिट्टी से निर्मित है तथा मृत्यु के पश्चात मिट्टी में ही विलीन होता है, मानव कुंभ (शरीर) भी कच्चा ही है, क्योंकि इसे संपत्ति आदि का अहंकार होता है। साथ ही मानव मन कामक्रोधादि अनेक स्वभाव दोषों से ओत-प्रोत होता है। इस प्रकार अनेक विकारों से युक्त देहरूपी कुंभ को रिक्त करने का सर्वोत्तम स्थल तथा काल है-कुंभ पर्व।
कुंभ मेले में नग्न नागा साधुओं की उपस्थिति भी महत्त्वपूर्ण है। यहाँ स्त्री-पुरुष लिंगभेद का विस्मरण होता है तथा कामवासना का विचार दूर ही रहता है।

कुंभ पर्व हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसमें सम्मिलित सभी ग्रंथ और संप्रदायों को – यह एकत्व के भाव में पिरोता है। इस दौरान भारतीय समाज की दशा एवं दिशा पर चिंतन किया जाता है। कौन-सी परंपरा समाज को हानि पहुँचा रही है, इसका विचार किया जाता है। इस मेले में कौन कहाँ से आया? किस जाति का है? किसको क्या पता और न ही जानने की किसी की इच्छा होती है। पवित्र नदियाँ सभी को नहला देती हैं। ऊँच-नीच, अमीर-गरीब के भावों से दूर सभी एक साथ स्नान करते हैं। सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा मंत्र यहीं मिलता है।
पूज्य संत मोरारी बापू जी कुंभ के आध्यात्मीकरण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि, ‘तन, मन व मति के दोषों की निवृति के लिए तीर्थ और कुंभ पर्व हैं।’ अमृत की प्राप्ति के लिए होने वाला देवासुर संग्राम हमारे भीतर ही हो रहा है। दैवीय और आसुरी वृत्तियों को विवेकरूपी मंदराचल का सहयोग लेकर मंथन करते-करते अपने चित्त रूपी सागर से चैतन्य का अमृत खोजने की व्यवस्था का नाम है-कुंभ पर्व। इस प्रकार का आत्मज्ञान और उसको पाने की युक्तियाँ सबको सहज में मिल जाएँ, इसीलिए कुंभ का पर्व है। कुंभ में संत-महात्माओं का सत्संग, सानिध्य मिलता है। उसका हेतु यह है कि मानव मन अपनी जन्म-जन्मांतरों की वासनाओं का अंत करके भगवद् सुख, शांति में सराबोर होकर विश्राति पाए। इस प्रकार मनुष्य के सर्वांगीण विकास की दूरदृष्टि रखने वाले भारत के ऋषि-मुनियों द्वारा सदियों से कुंभ परंपरा की सुरक्षा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस अवसर पर मनुष्य किन्हीं ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में पहुँचकर जीवन के वास्तविक अमृत की पावन गंगा में भी गोता लगा सके।
मार्क दुली के शब्दों में, ‘विश्व के सबसे विशाल जनसंगम के रूप में कुंभ एक चमत्कार ही है, भारत की अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति का दृश्य प्रतीक है।’ कुंभ मेला, वास्तव में विशाल भारत की ‘विविधता में एकता’ का संगम है। यह भारत के सांस्कृतिक प्रवाह के महान वाहक के रूप में उभरकर आता है। इस मेले में ज्योतिर्विज्ञान, आध्यात्म, इतिहास और जन-जीवन का अपूर्व संगम दिखाई देता है।
यह हमारे राष्ट्र निर्माण और समाज व्यवस्था का एक हिस्सा है, जो समाज को नित्य नूतन बनाए रखने में निरंतर सचेत रहता है। किसी भी समाज को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसमें नित्य नए-नए प्रयोग द्वारा समाज को एकजुट, समरस बनाए रखने, नई चेतना और ऊर्जा बनाए रखने की जरूरत होती है। समाज को चिरस्थायी बनाए रखने हेतु कुंभ पर्व भारतीय समाज का आधार है।
ऐसी भी मान्यताएँ हैं कि कुंभ की परंपरा का क्रमशः विकास हुआ है, जिसमें गोदावरी, क्षिप्रा, गंगा और त्रिवेणी के पवित्र तट पर किन्हीं विशेष राशि योग पर स्नान के निमित्त परंपरा पहले से चली आ रही थी और उसे आगे चलकर एक पौराणिक कथा के माध्यम से एक श्रृंखला में पिरो दिया गया। किंतु अगर यह भी हो, तब भी इसके पीछे भारत की सांस्कृतिक चेतना और एकता को जाग्रत व सुदृढ़ करने की भावना ही अवश्य रही होगी।
Important Link
- पाठ्यक्रम का सामाजिक आधार: Impact of Modern Societal Issues
- मनोवैज्ञानिक आधार का योगदान और पाठ्यक्रम में भूमिका|Contribution of psychological basis and role in curriculum
- पाठ्यचर्या नियोजन का आधार |basis of curriculum planning
राष्ट्रीय एकता में कौन सी बाधाएं है(What are the obstacles to national unity) - पाठ्यचर्या प्रारुप के प्रमुख घटकों या चरणों का उल्लेख कीजिए।|Mention the major components or stages of curriculum design.
- अधिगमकर्ता के अनुभवों के चयन का निर्धारण किस प्रकार होता है? विवेचना कीजिए।How is a learner’s choice of experiences determined? To discuss.
- विकास की रणनीतियाँ, प्रक्रिया के चरण|Development strategies, stages of the process
Disclaimer: chronobazaar.com is created only for the purpose of education and knowledge. For any queries, disclaimer is requested to kindly contact us. We assure you we will do our best. We do not support piracy. If in any way it violates the law or there is any problem, please mail us on chronobazaar2.0@gmail.com

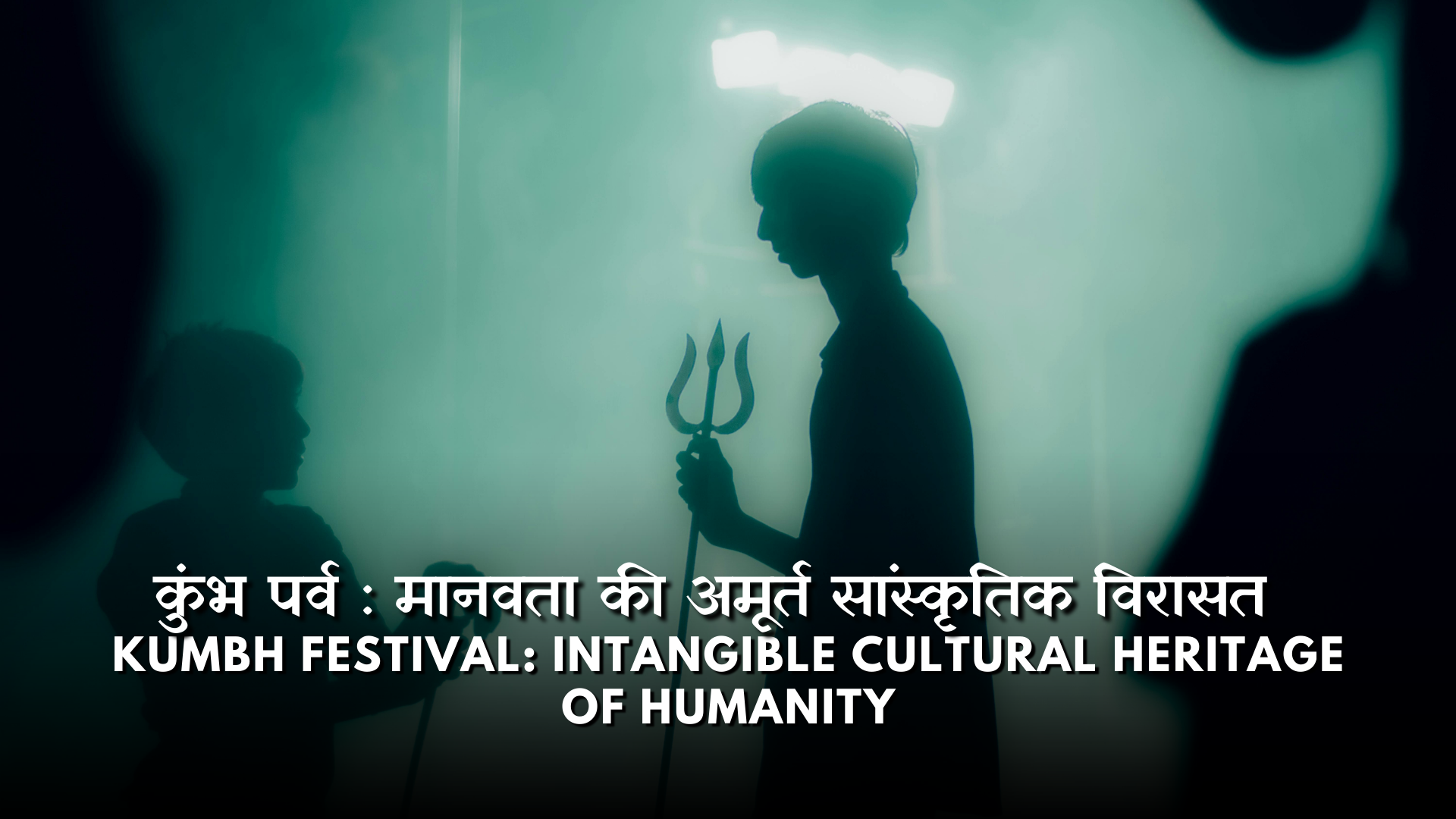

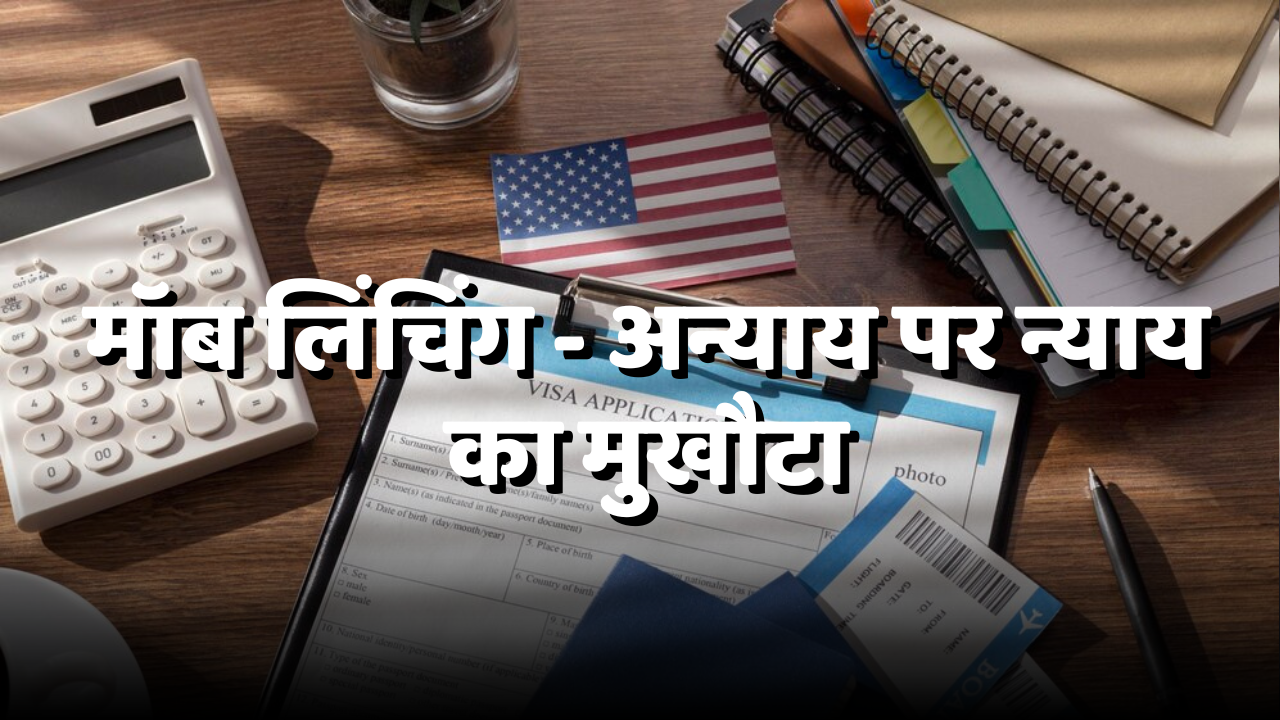

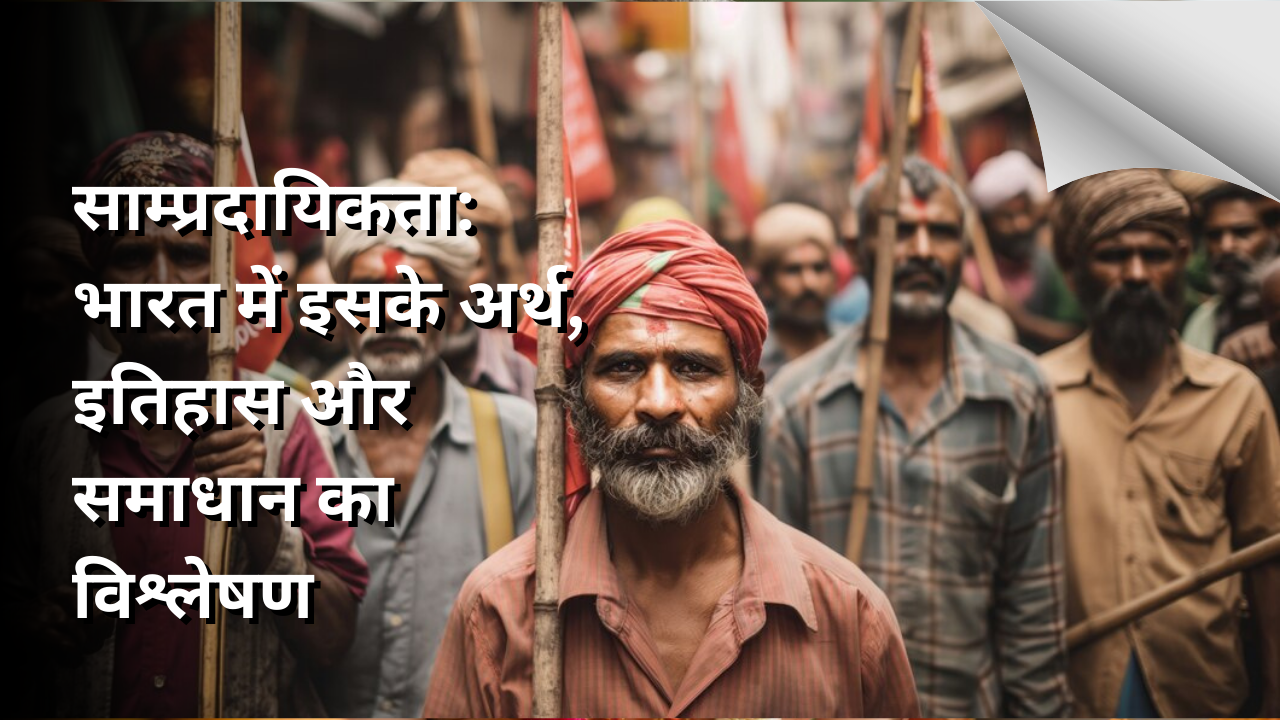



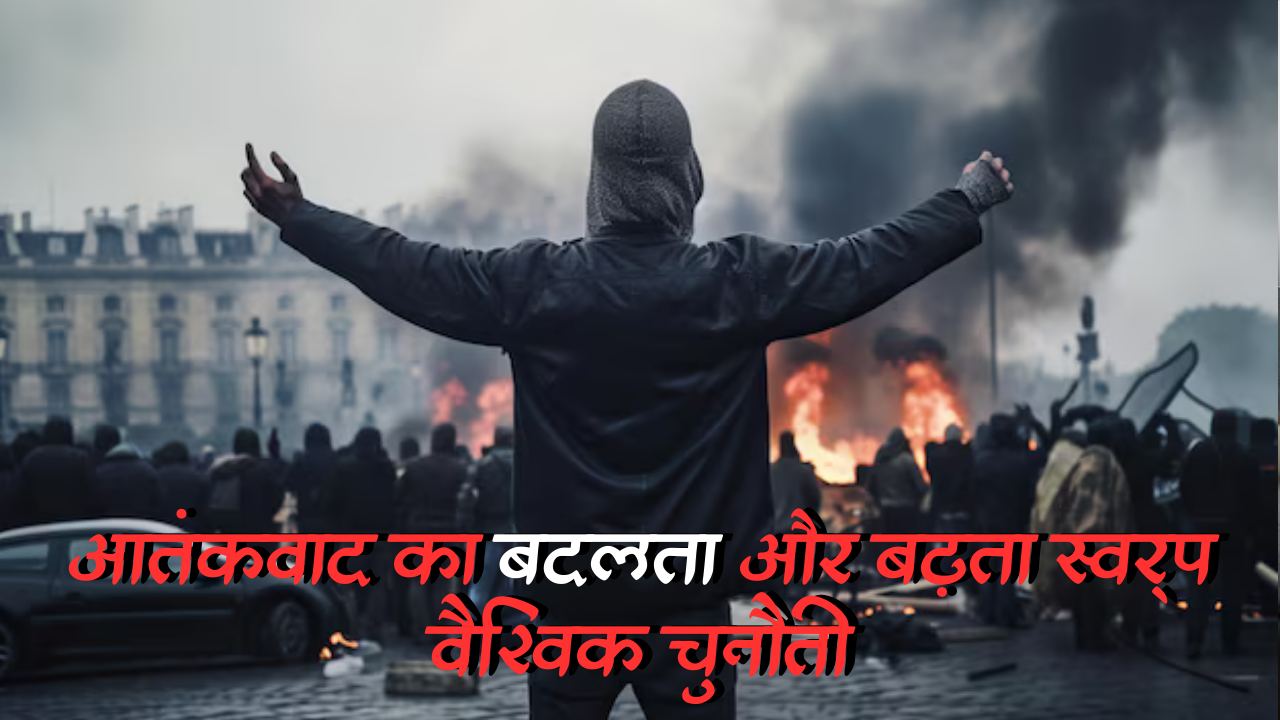
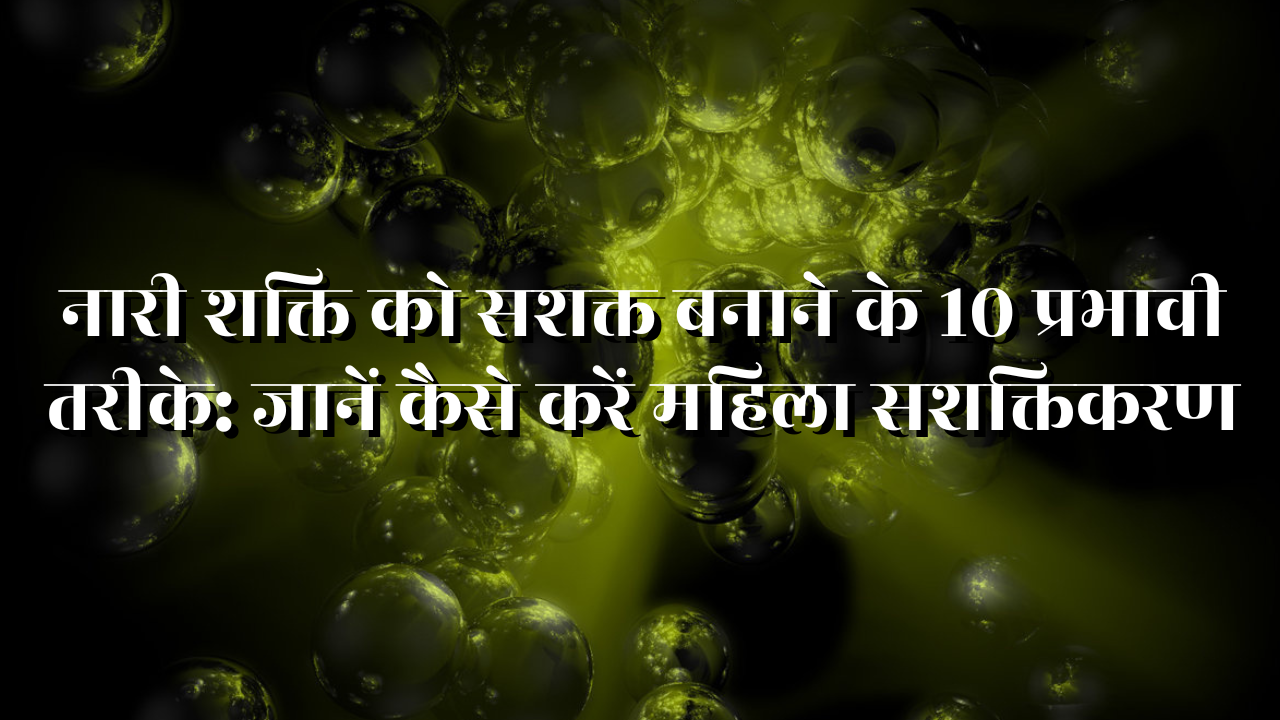
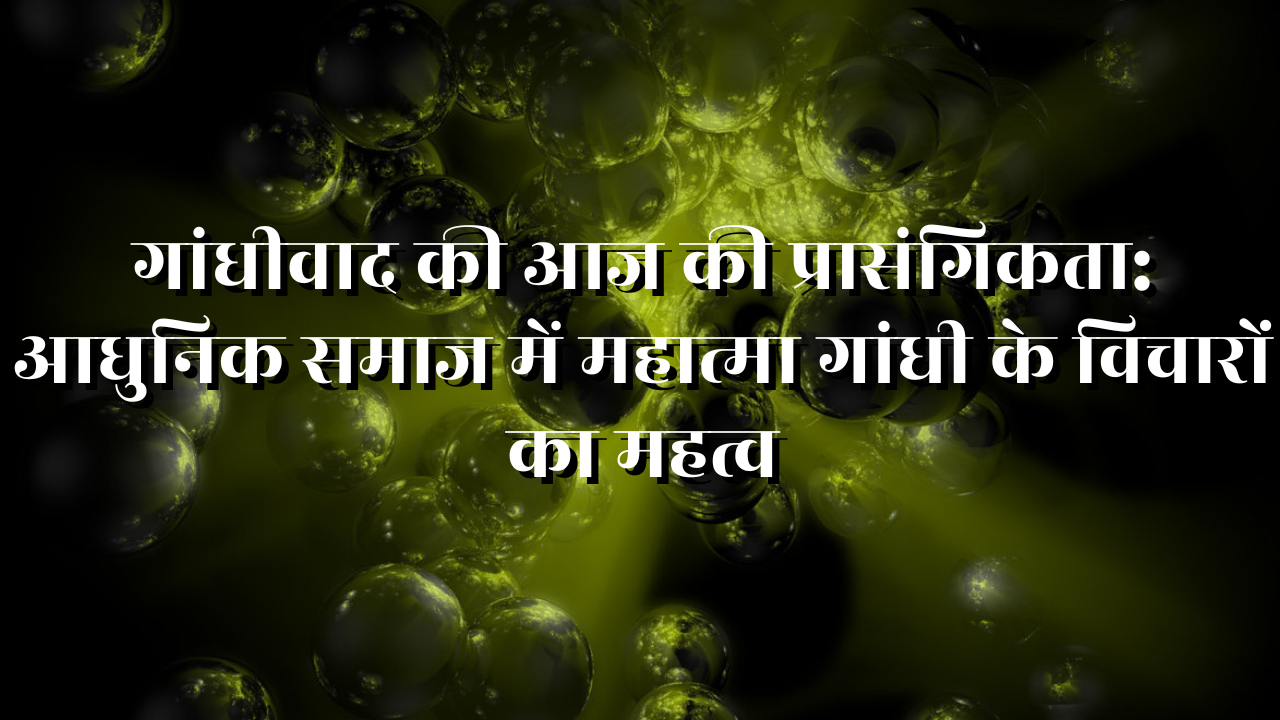

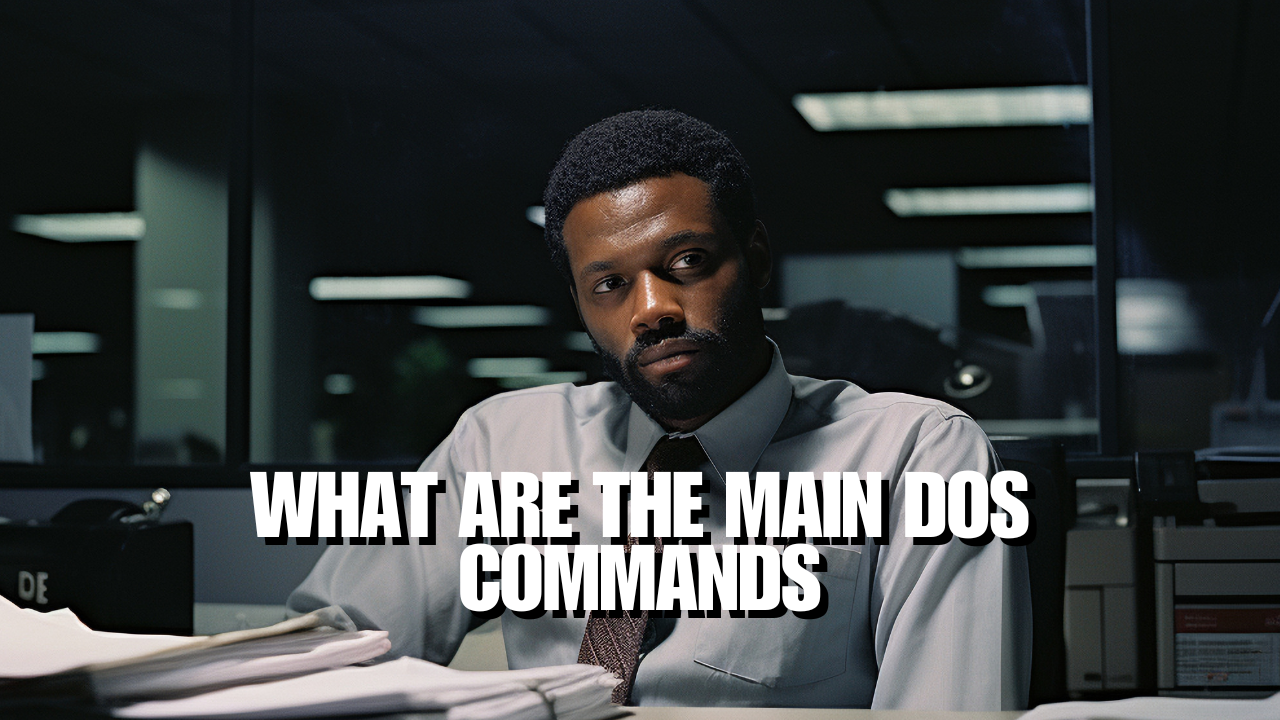
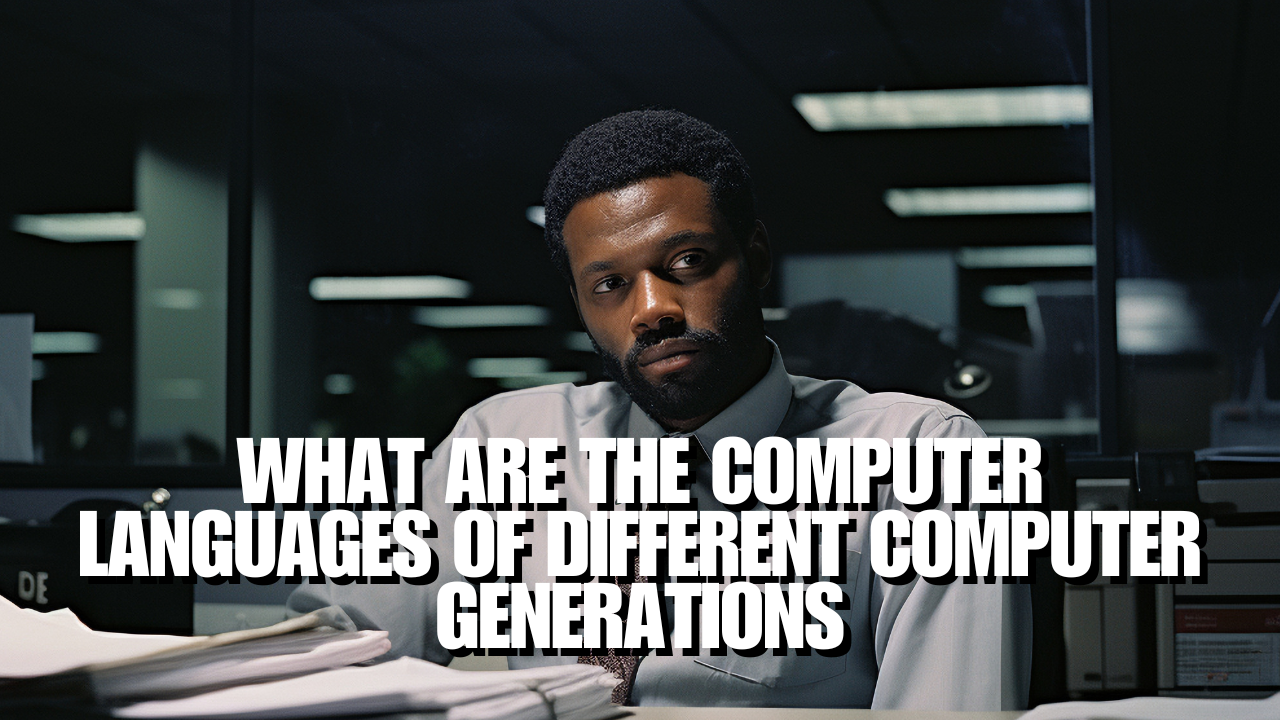

Leave a Reply